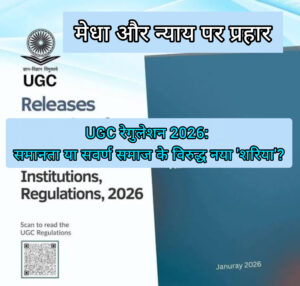सफ़ेद कमीज़, तिरंगा हाथ में,
वो सुबह निराली होती थी,
अश्विनी! तब देश की भक्ति,
बूंदी वाली थाली होती थी।
पाउच में जब मिलती बूंदी,
या छोटी सी वो एक जलेबी,
लगता था मिल गई हमें,
दुनिया की सारी ही मुट्ठी जेबी।
वो खीरे का टुकड़ा छोटा,
गाजर की फाँक निराली थी,
गणतंत्र की असली रौनक,
उसी एक पुड़िया वाली थी।
फिर २०१४ आया तो लगा कि
ये समानता का इक पर्व है,
हमें नागरिक होने का अब,
होता बड़ा ही गर्व है।
बहस बढ़ी, भाषण बढ़े,
और टीवी पर शोर बढ़ा,
२०२३ में जाकर देखो,
विमर्शों का ये ज़ोर बढ़ा।
पर २०२६ में खड़े होकर,
जब ‘मन’ की ओर मुड़ता है,
सारा ‘सिस्टम’ भारी-भारी,
अब आँखों में गड़ता है।
लगता है कि बचपन की,
वो सोच ही सबसे सच्ची थी,
वो बूंदी वाली बात ही देखो,
सबसे अच्छी और पक्की थी।
बाकी सब तो उलझन है,
बस शब्दों के खेल है,
बूंदी की मिठास के आगे,
सारा सिस्टम’ फेल है।
विद्यावाचस्पति अश्विनी राय ‘अरुण’