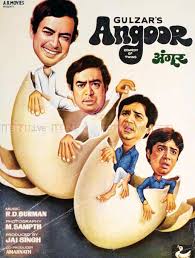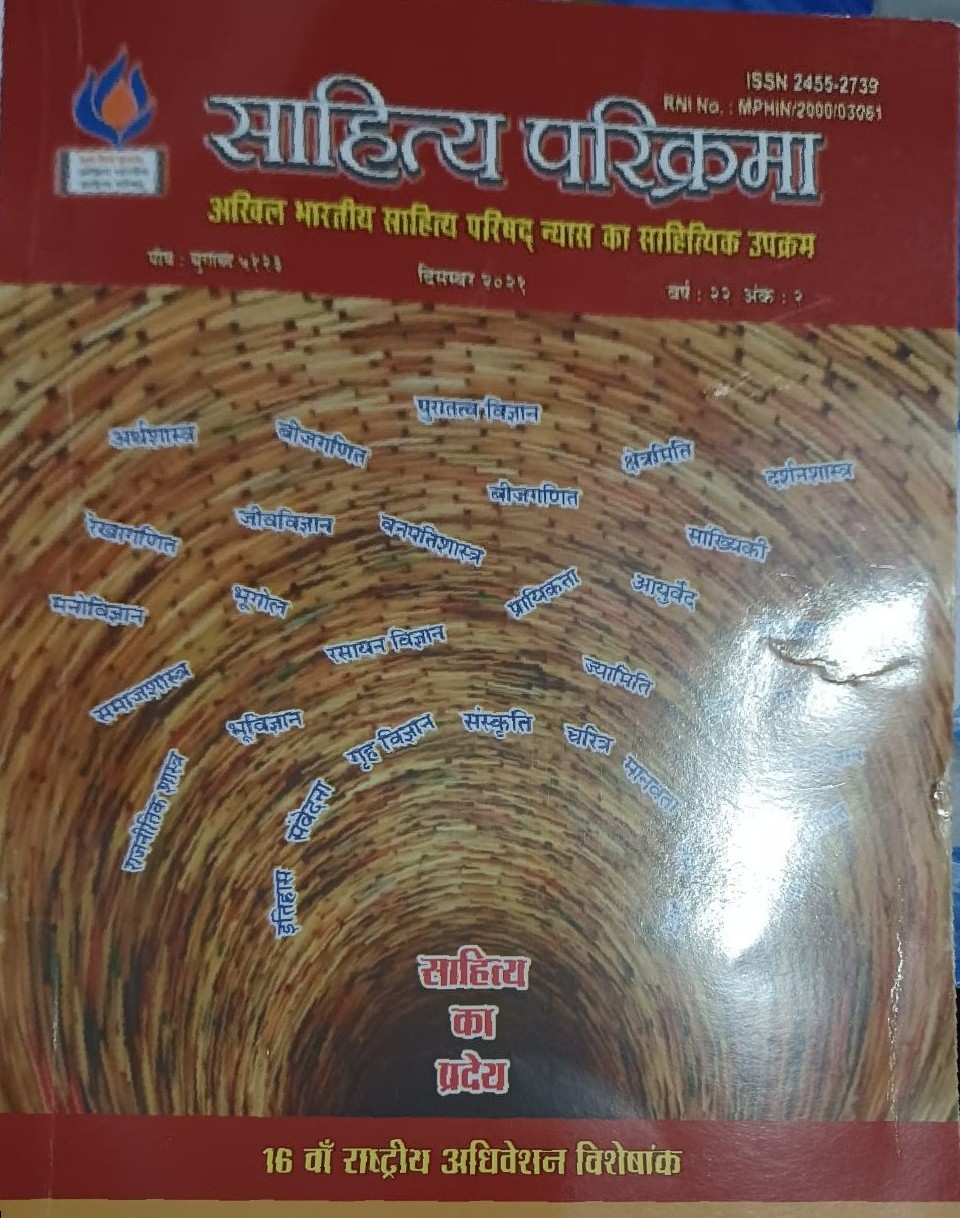
विषय : साहित्य का प्रदेय
शीर्षक : जीवन/समाज में साहित्य का योगदान
लेखक : अश्विनी राय ‘अरूण’
ग्राम : मांगोडेहरी, डाक : खीरी, जिला : बक्सर, बिहार।
यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान समय मे साहित्य का स्थान जनमानस के लिए क्या है। पहले शिक्षा, संस्कार के अलावा मनोरंजन का भी सर्वाधिक प्रचलित साधन साहित्य ही हुआ करता था। साहित्य से अधिक प्रभावशाली और आम जनता तक सरलता से पहुंचने वाला माध्यम और कोई नहीं था और देखा जाए तो आज भी नहीं है। कहते हैं कि गीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है जो की साहित्य की देन है। साहित्य ने व्यक्ति के जीवन के हर आयामों को छुआ है फिर चाहे वो सामाजिक हो, राजनितिक हो, धार्मिक हो, या आध्यात्मिक हो। जब से समाज की परिकल्पना की गई या यूं कहें कि सभ्य समाज बना वह साहित्य के अभिर्भाव से ही संभव हुआ। साहित्य के माध्यम से समाज में चल रही सामाजिक कुरीतियों को जनता के मध्य पेश किया गया और उन्हें जागरूक भी क्या गया। तो आइए पहले हम साहित्य को जान लेते हैं उसके बाद उसके प्रदेय पर बात करेंगे यानी जो प्रदान किये जाने के योग्य हो अथवा जो दिया जा सके। यानी साहित्य ने क्या दिया है इस पर चर्चा करेंगे। विद्वानों के अनुसार, ‘किसी भाषा के वाचिक और लिखित (शास्त्र समूह) को साहित्य कह सकते हैं।’ दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य – स+हित+य के योग से बना है। जिसका मतलब है कि सहित या साथ होने की अवस्था अथवा शब्द और अर्थ की सहितता यानी सार्थक शब्द। इसे यूं भी समझ सकते हैं, सभी भाषाओं में गद्य एवं पद्य की वे समस्त पुस्तकें जिनमें नैतिक सत्य और मानवभाव बुद्धिमत्ता तथा व्यापकता से प्रकट किए गए हों यानी वाङ्मय। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विषय के ग्रंथों का समूह यानी शास्त्र। किसी एक स्थान पर एकत्र किए हुए लिखित उपदेश, परामर्श या विचार आदि यानी लिपिबद्ध विचार या ज्ञान। सारांश में कहें तो साहित्य समस्त शास्त्रों एवम ग्रंथों का समूह है।
विद्वानों के अनुसार, भारत का संस्कृत साहित्य ऋग्वेद से आरम्भ होता है। व्यास, वाल्मीकि जैसे पौराणिक ऋषियों ने महाभारत एवं रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की। भास, कालिदास एवं अन्य कवियों ने संस्कृत में नाटक लिखे। भक्ति साहित्य में अवधी में गोस्वामी तुलसीदास, ब्रज भाषा में सूरदास तथा रैदास, मारवाड़ी में मीराबाई, खड़ीबोली में कबीर, रसखान, मैथिली में विद्यापति आदि प्रमुख हैं। अवधी के प्रमुख कवियों में रमई काका सुप्रसिद्ध कवि हैं। उसी तरह हिन्दी साहित्य में कथा, कहानी और उपन्यास के लेखन में प्रेमचन्द जी का महान योगदान है। अगर विदेशों की बात करें तो ग्रीक साहित्य में होमर के इलियड और ऑडसी विश्वप्रसिद्ध हैं। अंग्रेज़ी साहित्य में शेक्स्पियर के नाम को कौन नहीं जानता। और आज; साहित्य अपनी मुख्य धारा से हटकर व्यावसायिक पोखर में सिमट कर रह गया है, और वो भी बस आवश्यकता पड़ने पर। अगर इसे समझना हो तो उदाहरण के लिए महाभारत के पटकथा लेखक डा० राही मासूम रजा के शब्दों से समझा जा सकता है, ‘यह हिन्दी सिनेमा की बदनसीबी है कि हिन्दी सनेमा आज उन लोगों के हाथों में पल रहा है जिनका हिन्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो न हिन्दी लेखकों से परिचित हैं, न हिन्दी की उन बहुचर्चित कृतियों से, जिन पर बहुत अच्छी फिल्में बन सकती हैं। और यह स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हिन्दीभाषी निर्माता-निर्देशक नहीं होंगे जिन्होंने हिन्दी की कृतियों को अगर पढ़ा न भी हो तो उनकी चर्चा जरूर सुनी होगी और स्वाभाविक तौर पर उनका झुकाव ‘ओरीजनल’ विषयों की ओर होगा। आज हिंदी सिनेमा अपंग बन कर जी रहा है। उसके दोनों गढ़ बंबई और मद्रास अहिन्दी भाषी प्रदेश हैं और हिन्दी साहित्य के मध्य वह दरार है जो पट नहीं पा रही। वे हिन्दी लेखक चाहते हैं तो मात्र अनुवाद के लिए।
वैसे तो साहित्य का वृहद् रूप है चाहे वो किसी भी भाषा में ही क्यूं ना हो। उसने समाज को काफी कुछ दिया है। अगर आजीविका की बात की जाए तो इसके माध्यम से आज भी करोड़ो लोगो की आजीविका चलती है, हिंदी साहित्य को ही लें तो, भारतीय सिनेमा को ना केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत की आज़ादी के पश्चात साहित्य पर आधारित अनेकों सिनेमा बनीं जिन्होंने लोगो के दिलों पर राज किया जैसे; तमस, गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, तीसरी कसम, सूरज का सातवां घोड़ा, पति पत्नी और वो आदि।
देशभक्ति भी साहित्य की ही देन है। गीतों ने, कविताओं ने देश भक्ति की मशाल को जलाए रखा है। आज भी जब हम पुराने देशभक्ति गीत सुनते हैं तो उसी वक़्त मन देशभक्ति कि भावना से ओत प्रोत हो जाता है। साहित्य ने अपनी कहानियों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित रखने का सफलतम प्रयास किया है।
साहित्य के पदचिन्हों को आधार मानकर समाज अपने कदम आगे करता है और समाज अपने अनुभवों से साहित्य की रचना करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य मनुष्य के जीवन में सकरात्कम बदलाव लाने के साथ साथ उसमे कुछ कर गुजरने की चाह को भी आगे बढ़ाती है। इस परिपेछ्य में प्रेमचंद्र की एक कहानी नमक का दारोगा पर बात अपनी बात रखूंगा। नमक का दरोगा कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। कहानी के नायक मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिशाल कायम करता है। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। जिनकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी। अधिकांश अधिकारी उनके अहसान तले दबे हुए थे। अलोपीदीन ने धन के बल पर सभी वर्गों के व्यक्तियों को गुलाम बना रखा था। दरोगा मुंशी वंशीधर उसकी नमक की गाड़ियों को पकड़ लेता है, और अलोपीदीन को अदालत में गुनाहगार के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक आधिकारी उसे निर्दोष साबित कर देते हैं, जिसके बाद वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। इसके उपरांत पंडित अलोपीदीन, वंशीधर के घर जाके माफी मांगता है और अपने कारोबार में स्थाई मैनेजर बना देता है तथा उसकी ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाता है। मैं हर व्यक्ति को अपने बच्चों के साथ सभी परिजनों को ये कहानी पढ़ने की सलाह दूंगा। इस कहानी के माध्यम से ये सन्देश देने की कोशिश की गयी है कि ईमानदारी कभी आसान नहीं होती किंतु मूल्यवान होती है। यह तो नहीं पता की एक कहानी जब छपी होगी तब लोगो पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में जब इस पर फिल्म बने, नाटक प्रस्तुत हो अथवा इसे पढ़ा जाए तो निश्चित ही इसका प्रभाव स्थाई साबित होगा।
वर्तमान समय में साहित्य का स्वरुप पहले की अपेक्षा काफी बदल गया है, अब साहित्य का उद्देश्य सिर्फ अधिक से अधिक धन उपार्जन रह गया है, प्रकाशक अथवा संपादक को यह फर्क नहीं पड़ता की प्रस्तुत साहित्य का जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वह सकरात्मक है अथवा नकरात्मक। अब साहित्य सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय बन कर रह गया है जहाँ लेखकों के साथ पाठको की भावनाओं एवं संवेदनाओं को बिलकुल नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, आज भी जब हम पुरानी पुस्तकों के कहानियों को पढ़ते हैं अथवा कविताओं का गान करते हैं तो वह हमारे अंतर्मन को झंकृत कर देते हैं। अगर हम किसी पुराने फिल्मों के गीत को सुनते हैं तो उसे गुनगुनाने लगते है परन्तु वर्तमान में आयी कितनी रचनाओं को हम याद रख पाते हैं। जबकि आए दिन होने वाले साहित्यिक सम्मेलनों में हम पुस्तक विमोचन के उपरांत मुफ्त पुस्तक पाते हैं मगर कितनी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं। हां इनमे सिर्फ पुस्तकों का ही दोष नहीं है, मुफ्त में मिलने वाली पुस्तकों का हम महत्व भी नहीं समझते हैं और साथ ही पढ़ने की वह पहले वाली इच्छा भी नहीं रह गई है। मैं तो यह मानता हूँ की आजकल लोगो का नजरिया साहित्य को लेकर बदल गया है, लोग पुस्तकों को केवल और केवल सजावट का साधन मात्र मानते है, उन्हें ये बिलकुल फर्क नहीं पड़ता की लेखक ने इस पुस्तक को लिखने में कितनी मेहनत की है और प्रकाशक ने पुस्तक को छापने और पाठक तक पहुंचाने में कितना धन और समय व्यय किया है।
हालांकि आज के तनावग्रस्त वातावरण में लोगो को मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है और इसे पूरा करने के लिए साहित्य से अच्छा कोई ओर माध्यम नहीं है, परन्तु जिस प्रकार स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन का चुनाव करते हैं ठीक उसी प्रकार हमे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए साहित्य को चुनने की आवश्यकता है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साहित्य ने मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अतः प्रकाशक, संपादक, लेखकों को यह बात ध्यान रखना चहिए कि जो वह समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं क्या वो तर्कसंगत है अथवा क्या वह मनुष्य के जीवन में सकरात्मक प्रभाव ला सकता है, जो सामाजिक विकास में हितकर हो।