
हम बात शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य से, जिन्होंने घोषणा की थी कि जो दिखाई देने वाली दुनिया है वह सिर्फ झूठ है। अगर कुछ सत्य है, तो सिर्फ ब्रह्म है। उनके बाद आए रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा यहां खेल सिर्फ दो का नहीं तीन का है। पहली चेतन है, दूसरा अचित यानी जड़ तत्व और तीसरा इन दोनों को जोड़ने वाला ईश्वर। रामानुजाचार्य के बाद आते हैं मध्वाचार्य जी, जिन्होंने कहा, माया और ब्रह्म दोनों अलग हैं, दोनों कभी मिलते नहीं हैं। इसलिए न अद्वैत ठीक, न विशिष्टाद्वैत, सब तरफ सब समय द्वैत ही द्वैत है। फिर इसके बाद हुए आचार्य निंबार्क उन्होंने कहा, ‘द्वैत और अद्वैत दोनों की सत्ता है’ इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया द्वैताद्वैत। और फिर आए वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का परिचय दिया है।
वल्लभाचार्य…
वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुणधारा की कृष्णभक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टिमार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। जिनका जन्म सन् १४७९, वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मणभट्ट जी की पत्नी इलम्मागारू के गर्भ से काशी के समीप हुआ था। उन्हें ‘वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार’ कहा गया है। वे वेद शास्त्र में पारंगत थे। श्री रुद्रसंप्रदाय के श्री विल्वमंगलाचार्य जी द्वारा इन्हें ‘अष्टादशाक्षर गोपाल मन्त्र’ की दीक्षा दी गई। त्रिदंड सन्न्यास की दीक्षा स्वामी नारायणेन्द्र तीर्थ से प्राप्त हुई। विवाह पंडित श्रीदेव भट्ट जी की कन्या महालक्ष्मी से हुआ, और यथासमय दो महान तेजस्वी पुत्र हुए- श्री गोपीनाथ व विट्ठलनाथ।
जिनमें गोपीनाथ काशी के महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार के शोभा बने। गोपीनाथ ने ‘महाभारत दर्पण’ के ‘भीष्मपर्व’, ‘द्रोणपर्व’, ‘स्वर्गारोहणपर्व’, ‘शांतिपर्व’ तथा ‘हरिवंशपुराण’ का अनुवाद किया।
विट्ठलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और ‘अष्टछाप’ के संस्थापक थे। उन्होंने अपने पिता के चार शिष्य कुंभनदास, महाकवि सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास तथा अपने चार शिष्य चतुर्भुजदास, गोविन्द स्वामी, छीतस्वामी और नंददास को मिलाकर ‘अष्टछाप’ की स्थापना की। इतना ही नहीं विट्ठलनाथ ने तानसेन, रसखान और अछूत मोहन को भी उपदेश दिया था।
जन्म कथा…
श्री लक्ष्मणभट्ट अपने संगी-साथियों के साथ यात्रा के कष्टों को सहन करते हुए जब वर्तमान मध्य प्रदेश में रायपुर ज़िले के चंपारण्य नामक वन में होकर जा रहे थे, तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रसव-पीड़ा होने लगी। सांयकाल का समय था। सब लोग पास के चौड़ा नगर में रात्रि को विश्राम करना चाहते थे; किन्तु इल्लमा जी वहाँ तक पहुँचने में भी असमर्थ थीं। अतः लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी सहित उस निर्जंन वन में रह गये और उनके साथी आगे बढ़ कर चौड़ा नगर में पहुँच गये। उसी रात्रि को इल्लम्मागारू ने उस निर्जन वन के एक विशाल शमी वृक्ष के नीचे अठमासे शिशु को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निष्चेष्ट और संज्ञाहीन सा ज्ञात हुआ, इसलिए इल्लम्मागारू ने अपने पति को सूचित किया कि मृत बालक उत्पन्न हुआ है। रात्रि के अंधकार में लक्ष्मण भट्ट भी शिशु की ठीक तरह से परीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने दैवेच्छा पर संतोष मानते हुए बालक को वस्त्र में लपेट कर शमी वृक्ष के नीचे एक गड़ढे में रख दिया और उसे सूखे पत्तों से ढक दिया। तदुपरांत उसे वहीं छोड़ कर अपनी पत्नी सहित चौड़ा नगर में जाकर रात्रि में विश्राम करने लगे।
दूसरे दिन प्रात:काल यात्रियों ने बतलाया कि काशी पर यवनों की चढ़ाई का संकट दूर हो गया है। उस समाचार को सुन कर उनके कुछ साथी काशी वापिस जाने का विचार करने लगे और शेष दक्षिण की ओर जाने लगे। लक्ष्मण भट्ट काशी जाने वाले दल के साथ हो चल दिए। जब वे गत रात्रि के स्थान पर पहुंचे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र को जीवित अवस्था में पाया। ऐसा कहा जाता है उस गड़ढे के चहुँ ओर प्रज्जवलित अग्नि का एक मंडल सा बना हुआ था और उसके बीच में वह नवजात बालक खेल रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देख कर दम्पति को बड़ा आश्चर्य और हर्ष हुआ। इल्लम्मा जी ने तत्काल शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और स्नेह से स्तनपान कराया। उसी निर्जन वन में बालक के जातकर्म और नामकरण के संस्कार किये गये। बालक का नाम ‘वल्लभ’ रखा गया, जो बड़ा होने पर सुप्रसिद्ध महाप्रभु वल्लभाचार्य हुआ। उन्हें अग्निकुण्ड से उत्पन्न और भगवान की मुखाग्नि स्वरूप ‘वैश्वानर का अवतार’ माना जाता है।
शुद्धाद्वैत सिद्धांत…
शुद्धाद्वैत के संदर्भ में वल्लभाचार्य द्वारा भागवत पर रचित सुबोधिनी टीका का महत्त्व बहुत अधिक है। उनके अनुसार ब्रह्म के तीन रूप हैं, पहला आधिभौतिक, दूसरा आध्यात्मिक और तीसरा आधिदैविक। आधिभौतिक ब्रह्म क्षर पुरुष है, वही प्रकृति या जगतरूप है। आध्यात्मिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। जबकि आधिदैविक ब्रह्म परब्रह्म है। क्षर पुरुष से अक्षर ब्रह्म और अक्षर से भी श्रेष्ठ है परब्रह्म। इसी ब्रह्म को गीताकार ने पुरुषोत्तम ब्रह्म कहा है।
वल्लभाचार्य ने कारण और कार्य को अलग-अलग न मानते हुए एक उदाहरण दिया है कि एक लपेटा हुआ वस्त्र या सूत का गोला छोटे से छोटा हो सकता है मगर जैसे ही उसे खोलना या घसीटना शुरू करो तो यही गोला विस्तीर्ण होता चला जाता है। ठीक इसी तरह आविर्भाव दशा में जगत और तिरोभाव दशा में ब्रह्म है। उत्पत्ति, स्थिति और लय हो जाने वाला यह जगत सही अर्थों में प्रभु की लीला है। लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। कार्य की निण्णत्ति हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। जब सब कुछ हो रहा हो और होने के साथ-साथ कुछ भी नहीं हो रहा हो, यानी बार बार होकर भी बार बार न होता चले तो उसे लीला कहते हैं। अगर सीधी बातों में कहें तो लीला का अर्थ होता है, खेल, खिलवाड़, क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन आदि। जिसमें होता तो सब कुछ है, मगर उसका सही मायनों में देखा जाए तो खेल खत्म होने के बाद सब कुछ वैसे के वैसे ही रहता है, जो खेल शुरू होने से पूर्व था। आचार्य ने अपने सिद्धांत को पुष्टि मार्ग बताया। उन्होंने जीव तीन प्रकार के बताए हैं। पुष्टि जीव जो ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। दूसरे मर्यादा जीव, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं और तीसरे वे जीव जो संसार के प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं।
ग्रंथ…
१. ब्रह्मसूत्र का ‘अणु भाष्य’ और वृहद भाष्य’
२. भागवत की ‘सुबोधिनी’ टीका
३. भागवत तत्वदीप निबंध
४. पूर्व मीमांसा भाष्य
५. गायत्री भाष्य
६. पत्रावलंवन
७. पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम
८. दशमस्कंध अनुक्रमणिका
९. त्रिविध नामावली
१०. शिक्षा श्लोक
११ से २६ तक षोडस ग्रंथ – (१. यमुनाष्टक, २. बाल बोध, ३. सिद्धांत मुक्तावली, ४. पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, ५. सिद्धान्त, ६. नवरत्न, ७. अंत:करण प्रबोध, ८. विवेकधैयश्रिय, ९. कृष्णाश्रय, १०. चतुश्लोकी, ११. भक्तिवर्धिनी, १२. जलभेद, १३. पंचपद्य, १४. संन्सास निर्णय, १५. निरोध लक्षण १६. सेवाफल)
२७. भगवत्पीठिका
२८. न्यायादेश
२९. सेवा फल विवरण
३०. प्रेमामृत तथा
३१ से ३८ तक विविध अष्टक– (१. मधुराष्टक, २. परिवृढ़ाष्टक, ३. नंदकुमार अष्टक, ४. श्री कृष्णाष्टक, ५. गोपीजनबल्लभाष्टक आदि।)
शिष्य परम्परा…
श्री वल्लभाचार्यजी के चौरासी शिष्यों के अलावा अनगिनत भक्त, सेवक और अनुयायी थे। उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी यानी गुसाईं जी ने बाद में उनके चार प्रमुख शिष्यों – भक्त सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास और कुम्भनदास, तथा अपने स्वयं के चार शिष्यों – नन्ददास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी तथा चतुर्भुजदास, जो सभी श्रेष्ठ कवि तथा कीर्तनकार भी थे, का एक समूह स्थापित किया जो “अष्टछाप” कवि के नाम से प्रसिद्ध है।
सूरदासजी की सच्ची भक्ति एवं पद-रचना की निपुणता देख अति विनयी सूरदास जी को भागवत् कथा श्रवण कराकर भगवल्लीलागान की ओर उन्मुख किया तथा उन्हें श्रीनाथजी के मन्दिर की कीर्त्तन-सेवा सौंपी। उन्हें तत्व ज्ञान एवं लीला भेद भी बतलाया। जिसपर सूरदास जी कहते हैं, “श्रीवल्लभगुरू तत्त्व सुनायो लीला-भेद बतायो [सूरसारावली]।
भरोसो दृढ इन चरनन केरो। श्रीवल्लभ-नख-चंद्र-छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो॥
श्रीवल्लभ जी के प्रताप से प्रमत्त कुम्भनदास जी तो सम्राट अकबर तक का मान-मर्दन करने में नहीं झिझके।
परमानन्ददास जी के भावपूर्ण पद का श्रवण कर महाप्रभु कई दिनों तक बेसुध पड़े रहे।
उपास्य श्रीनाथजी ने कलि-मल-ग्रसित जीवों का उद्धार हेतु श्रीवल्लभाचार्यजी को दुर्लभ आत्म-निवेदन-मन्त्र प्रदान किया और गोकुल के ठकुरानी घाट पर यमुना महारानी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया।
आसुरव्यामोह लीला…
विक्रम संवत् १५८७, आषाढ शुक्ल तृतीया (सन १५३१) को उन्होंने अलौकिक रीति से इहलीला संवरण कर सदेह प्रयाण किया, जिसे ‘आसुरव्यामोह लीला’ कहा जाता है। वैष्णव समुदाय उनका चिरऋणी है।




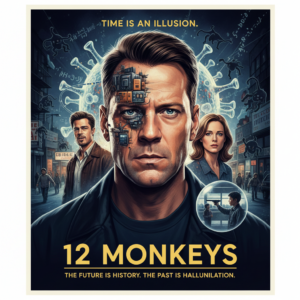
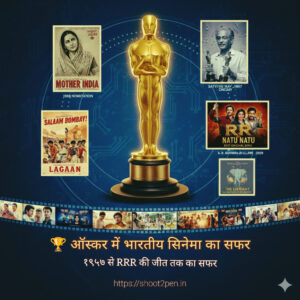

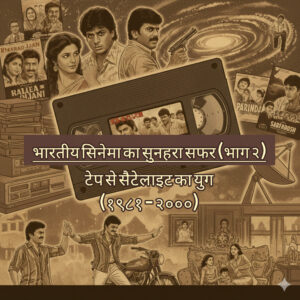
1 thought on “वल्लभाचार्य”