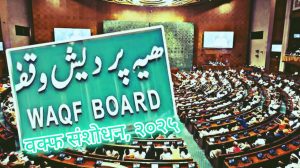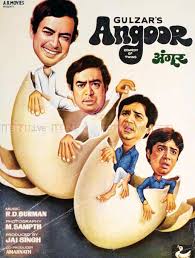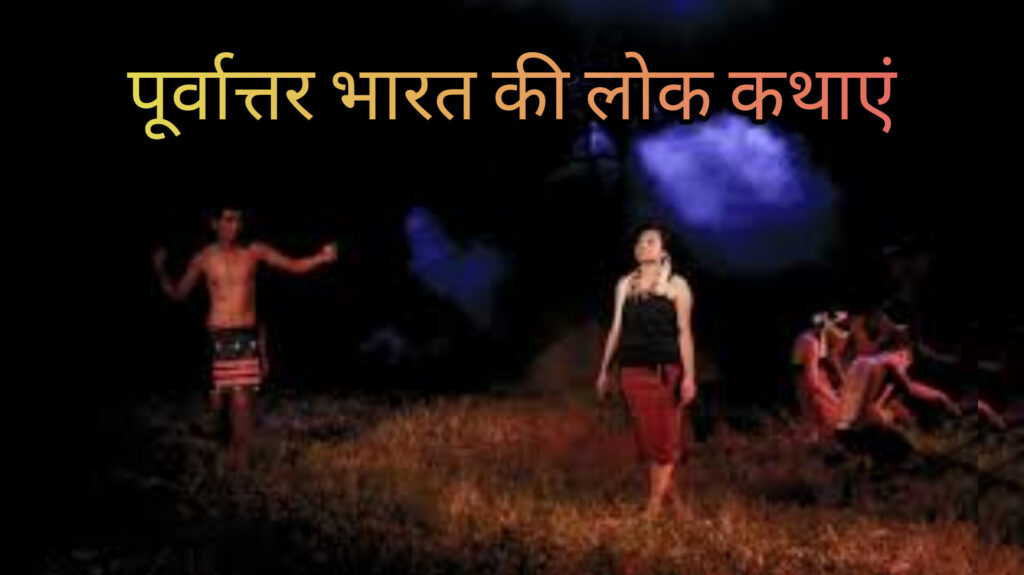
किसी भी देश अथवा समाज में साहित्य का आरंभ बहुत बाद में हुआ है, क्योंकि साहित्य के लिए लिपि, मानक भाषा, विचार व्यक्त करने की कला यानी कूल मिलाकर व्याकरण की आवश्यकता होती है। किंतु जहाँ तक लोक साहित्य की बात है, इसके लिए इन तत्त्वों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोग अपनी सामान्य भाषा में ही अपने आंतरिक भावों को लोक साहित्य के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि लोक साहित्य व्याकरणीय साहित्य की जननी होती है। बाद के समय में समाज में जो लिखित साहित्य का सृजन होता है, वह पुराने लोक साहित्य से ही कई बार प्रेरित होता है अथवा तत्वों को ग्रहण करता है। लोक-साहित्य लिखित नहीं होता बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक ही हस्तांतरित होता चला जाता है। आजकल इसकी चर्चा कम होने की वजह से हो अथवा संरक्षित करने की भावना के कारण ही हो लोक साहित्य का लिखित रूप भी सामने आने लगा है।
जहाँ तक पूर्वोत्तर भारत की बात है, यहाँ विभिन्न समय विभिन लोगों की जनगोष्ठियों का प्रभाव देखा जाता है। यह प्रभाव भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज, उत्सव, चीजों के नाम आदि सभी में स्पष्ट परिलक्षित होता है अथवा यह कहना अधिक उचित होगा कि नेग्रिटो, ऑष्ट्रिक, द्रविड़, मंगोल आदि के साथ-साथ सभी जनजातीय संस्कृति के संमिश्रण से वृहद पूर्वोत्तर भारत का गठन हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित लोक साहित्य की बात की जाये तो लिखित साहित्य के साथ-साथ लोकसाहित्य की भी यहाँ कमी नहीं है। इसमें सामान्य जनमानस के भावावेग, अनुभूति, सुख-दु:ख के क्षण, विश्वास, परंपरा आदि संस्कृति का विविध पक्ष मुखर हो उठा है। पूर्वोत्तर भारत के आठों राज्यों में सैंकड़ों जनजातियां रहती हैं। सबकी भाषा-संस्कृति अलग-अलग हैं। इसी के चलते लोक साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति में भी अंतर पायी जाती है। पूर्वोत्तर भारत लोक साहित्य का खान है। आज भी जिन जनजातियों की अपनी लिपि नहीं है अथवा लिखित साहित्य नहीं है वे लोक साहित्य में बहुत समृद्ध है। हर एक पेड़, पहाड़, नदी, पत्थर, जंगल, रास्ते के साथ उनकी कथा-कहानियों की, किंवदंतियों की सांस्कृतिक विरासत जुड़ी हुई है। सामान्य रूप से लोक साहित्य को छह भागों में बाँटा जाता है – क) कहानी, ख) गीत अथवा लोकगीत, ग) दृष्टांत, घ) मुहावरा, ङ) लोकोक्ति, च) मंत्र। इन भागों को फिर से कई उपभागों में भी विभाजित किया गया है। इसलिए आज लोककथा पर ही चर्चा की जाएगी…
नागालैंड का एक लोकगीत – एओ जनजाति की एक प्रेम कहानी…
यह लोकगीत अमर प्रेमकथा पर आधारित है, जो नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के मोपुंगचुकेट नामक एक पुराने गाँव में घटित होती है जहाँ एक प्रेमी जोड़ा जीना और एतिबेन रहते थे। जीना, एक गरीब आदमी था, जिसे एतिबेन से प्यार हो जाता है। एतिबेन एक अमीर परिवार से थी। दोनों प्रेमी छुप छुप कर कभी पहाड़ों में तो कभी झील के पास एक-दूसरे से मिलते। जब उनके माता-पिता और गाँव के लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो वे उनके रिश्ते का सख्त विरोध करने लगे। जब एतिबेन नहीं मानी तो उसके माता-पिता ने एतिबेन के लिए जीना से दहेज में गाय और बैलों की मांग की। चूंकि जीना गरीब था, इसलिए वह दहेज चुकाने में असफल रहा। इसी बीच, सुंगरात्सु गांव का तेन्युर नाम का एक अमीर आदमी गाय-बैलों के साथ वहां आया और उसने एतिबेन के माता-पिता से उसका हाथ मांगा। वे सहमत हो गए और एतिबेन का तेन्युर से शादी कर दी।
समाज की नजर में तो दोनों प्रेमी अलग हो गए थे मगर वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कृतसंकल्प थे, अतः गुप्त रूप से खेतों में वे एक-दूसरे से मिलते रहे। मगर एक दिन तेन्युर ने उन्हें पकड़ लिया। उसने एतिबेन को खूब पीटा जिससे वह बीमार रहने लगी। जीना को इसके बारे में जब पता चला तो उसने एतिबेन की बहुत सावधानी से देखभाल करने लगा। मगर एक दिन एतिबेन ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया यह देख जीना की भी जल्द ही मृत्यु हो गई। जब ग्रामीण उनके शवों को जला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दो धुएँ के रंग की आकृतियाँ हाथ पकड़े हुए आसमान में ऊपर उठ रही थीं जो जिना और एतिबेन से मिलती जुलती थीं।
विश्लेषण…
नागालैंड लोककथाओं की भूमि है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। यहां के संगीत उनके जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। यहां लोककथाओं और गीतों के माध्यम से मौखिक परंपरा को जीवित रखा गया है। उन्हीं में से है एओ जनजाति की प्रेम कहानी आधारित यह लोकगीत। यह लोकगीत रोमांटिक और ऐतिहासिक दोनों है, जिसमें जीना और एतिबेन की पूरी कहानी बताई गई है। वैसे तो यह एक मौसमी गीत है, जो किसी विशेष कृषि मौसम में गाई जाती है, लेकिन इसके गाने का ढंग रोचक और संगीतमय होता है। मगर अंत दुखद होने की वजह से कुछ समय तक दिलोदिमाग में इस तरह बस जाता है कि अपने आप में एक खालीपन सा महसूस होता है।
अरुणाचल प्रदेश की इदु मिश्मी जनजाति का लोकगीत आधारित एक लोककथा…
एक समय, दिबांग घाटी की पहाड़ियों में रहने वाले एक विवाहित जोड़े के घर एक खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ। जन्म के पांच दिन बाद भी, माता-पिता ने उसका नाम तय नहीं किया था, और तभी उन्होंने एक पक्षी को “अंची-अंची” गाते हुए सुना। उन्हें चिड़िया का चहचहाना बहुत पसंद आया और उसी के अनुरूप उन्होंने अपनी बेटी का नाम अंची रखा।
अंची जब बड़ी हुई तब उसकी शादी अंगोलिन गांव के एक युवक से हो गई। जब अंची अपने पति के घर जा रही थी, तभी एक खिनु (आत्मा) ने उसे पकड़ लिया। अंची हवा में तैरी और गायब हो गई। यह देख गांव वाले डर गए और इगु (इंग्लैंड:पुजारी) ने अपनी ईश्वर-प्रदत्त बुद्धि और अंतर्दृष्टि से पता लगाया कि अंची खिनु द्वारा सुझाया गया नाम था इसलिए वह उसकी है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता।
कई वर्ष बाद अंची जब अपने अपने माता-पिता के पास आई तो लोगों ने उसके आसपास असाधारण चीजें देखीं। एक दिन, वह अपने माता-पिता के लिए एक लाल कपड़ा और एक मुर्गा लेकर आई। उसने उनसे कहा कि जब तक वह जिंदा रहेगी, मुर्गा बड़ा होता रहेगा और कपड़ा भी दिखता रहेगा। पांच साल तक गांव वालों ने दूर की पहाड़ी पर धूप के दिनों में कपड़ा फैला हुआ देखा और मुर्गे की बांग भी सुनी। आखिर एक दिन ऐसा आ गया जब कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। तब सभी को विश्वास हो गया कि अंची अब हमेशा के लिए चली गई है। इसीलिए मध्य दिबांग घाटी में अंगोलिन और अप्रुली गांवों के बीच स्थित पहाड़ी को “नानी अंची अलोमी अको’ के नाम से जाना जाता है, जो आज भी स्थित है।
विश्लेषण…
अरुणाचल प्रदेश की इदु मिश्मी जनजाति की यह लोककथा प्रसव के बाद ५ दिनों के भीतर अपने नवजात शिशुओं का नामकरण करने की इदु परंपरा के पीछे की नैतिकता के बारे में बताती है। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो यह माना जाता है कि खिनु (इंग्लैंड:आत्मा) बच्चे का नाम रखेगी और उसे अपने साथ ले जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश की लोककथा – दुनिया कैसे बनी, इस पर एक सिंगफो जनजाति की कहानी…
आरंभ में न तो पृथ्वी थी और न ही आकाश। वहाँ सब कुछ बादल और धुंध था। इसी बादल और धुंध से खुपनिंग-कुआम नामक एक स्त्री का जन्म हुआ। चूँकि वह धुंध से आई थी अतः देखने में बिल्कुल बादल की तरह थी। कुछ समय बाद उसने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया जो बर्फ के समान थे। लड़के का नाम उसने तुंग-काम-वाइसुन रखा और लड़की का नाम उसने निंगोन-शिनुन रखा। जब दोनों बड़े हुए, तो उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली और जल्द ही उन्होंने इंगा (पृथ्वी) नामक एक लड़की और म्यू (आकाश) नामक एक बेटे को जन्म दिया। इंगा मिट्टी जैसी दिखती थी और म्यू , बादल जैसा। आख़िरकार इन दोनों ने भी शादी कर ली और इम्बुंग (हवा) नाम के एक लड़के को जन्म दिया। जब इम्बुंग पैदा हुआ तो उसने इतनी ज़ोर से अपने पिता को उड़ाया की वह आकाश में बादल बन गया। तथा अपनी माँ को सुखा दिया, जिससे वह मिट्टी बन गई। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ।
विश्लेषण…
यह लोककथा सिंगफो जनजातियों में सबसे अधिक कही और सुनी जाने वाली कहानियों में से एक है। सिंगफो जनजाति अरुणाचल प्रदेश के अलावा, चीन और म्यांमार में भी निवास करती है जहां उन्हें क्रमशः जिंगपो और काचिन के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति अपनी स्वतंत्रता, अनुशासित मार्शल आर्ट कौशल और अपनी जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जहां प्रकृति भी उनके साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः उनकी कथाओं में प्रकृत का प्रभाव सहज ही देखने सुनने को मिलता है। इस कथा को सुनने सुनाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है फिर भी ये वहां काफी प्रसिद्ध है।
मिजोरम का एक लोकगीत – रिह दिल झील…
यह किंवदंती है या सच्चाई कि किसी समय में रिही नाम की एक लड़की थी, जिसका दुर्भाग्य यह था कि वह क्रूर सौतेली माँ और पिता के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, उसके पिता ने रिही की छोटी बहन को जंगल में ले जाकर मार डाला। अपनी बहन का बेजान शरीर को देख रिही फूट-फूट कर रोने लगी। लासी नामक एक मित्रवत आत्मा ने रिही को रोते देखा तो उसने उसे एक जादुई पेड़ की शक्तियों के बारे में बताया जिसका उपयोग कर रिही ने अपनी मृत बहन को जीवित कर लिया। रिही अब जादुई पेड़ के पत्तों का उपयोग करके खुद को किसी भी चीज में बदल सकती थी। उसने बहन के प्यास को बुझाने के लिए पानी के एक छोटे से झील में बदल लिया। रिही के सम्मान में ही उस झील का नाम रिह पड़ा।
विश्लेषण…
इस लोककथा अंतर्गत आने वाली रिह झील, मनमोहक हरियाली के मध्य स्थित पूरे मिजोरम की सबसे बड़ी झील है। यह रिह झील देखने में दिल के आकार की है, इसलिए इसे रिह दिल झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में अजीब बात यह है कि यह म्यांमार में स्थित है। लेकिन शायद इसका संबंध मिज़ो लोगों की संस्कृति और परंपरा पर झील का प्रभाव से है। ऐसा माना जाता है कि मृतकों की आत्माएं मिट्ठी खुआ के अगले निवास के रास्ते में इसे अनिवार्य रूप से पार करती हैं, और कुछ लोग इसे सभी आत्माओं का अंतिम घर भी मानते हैं। आपके जानकारी के लिए बताते चलें कि इस झील ने ना जाने कितने समय से मिजोरम के लेखकों और संगीतकारों को प्रभावित और उन्हें समृद्ध किया है।
अपनी बात…
इन लोक कथाओं के अलावा भी वर्णनमूलक कथा, किंवदंती अथवा जनश्रुतिमूलक कथा, दु:ख-दैन्य के कथा आदि लोककथा भी पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित हैं। ये सारी लोककथाएं केवल मात्र कहानियां नहीं बल्कि पूरे समाज की अभिव्यक्ति है। इससे एक समाज की कथा, किंवदंती आदि परंपराओं को जाना जा सकता है। इससे ही एक समाज का स्वकीय परिचय का निर्माण होता है। वास्तव में कहा जाए तो ये समाज के इतिहास हैं और हमारे धरोहर हैं।