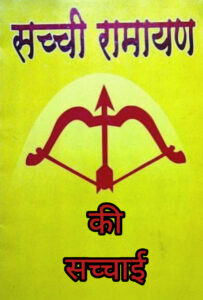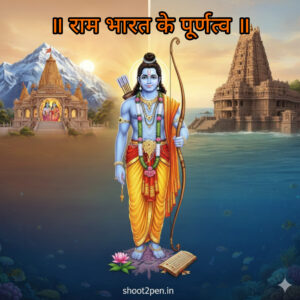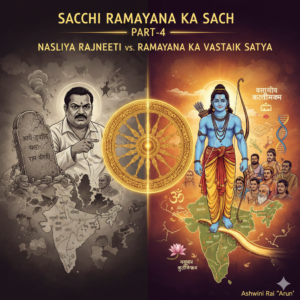I. ‘आत्मकथ्य’ का केंद्रीय भाव और संक्षिप्त सार
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘हंस’ के ‘आत्मकथा विशेषांक’ के लिए छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से जब आत्मकथा लिखने का आग्रह किया गया, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया। ‘आत्मकथ्य’ कविता इसी अस्वीकृति और उसके पीछे के तर्कों का शालीन आत्म-निवेदन है।
कवि भौंरे (मन) के माध्यम से अपनी कथा कहने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका जीवन सुखों से रहित होकर पतझड़ जैसा हो गया है। वे तर्क देते हैं कि हिंदी साहित्य के इस विशाल आकाश में महान लेखकों की आत्मकथाएँ पढ़कर लोग उनकी दुर्बलताओं का उपहास करते हैं। कवि नहीं चाहते कि उनकी ‘खाली गागर’ (सुख रहित जीवन) को देखकर उनके मित्र उपहास करें या यह समझें कि उन्होंने ही उनके जीवन के आनंद को छीन लिया था।
कवि अपने सरल स्वभाव के कारण हुए धोखों और अपने निजी, प्रेम भरे क्षणों (‘उज्ज्वल गाथा’) को सार्वजनिक करके उनका अपमान नहीं करना चाहते। उनकी प्रिय पत्नी के साथ बिताए मधुर क्षणों की स्मृतियाँ ही अब उनके थके हुए जीवन का एकमात्र ‘पाथेय’ (सहारा) हैं। कवि मानते हैं कि उनके छोटे से जीवन में सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसलिए वे चुप रहकर दूसरों की कहानियाँ सुनना अधिक उचित मानते हैं। अंत में, वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, क्योंकि उनका दुःख अब शांत होकर सो गया है और वे उसे फिर से कुरेदकर दुखी नहीं होना चाहते।
II. ‘आत्मकथ्य’ के काव्यांशों की गहन व्याख्या
काव्यांश १
मधुप गुन–गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी,
मुरझाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी।
इस गंभीर अनंत–नीलिमा में असंख्य जीवन–इतिहास
यह लो, करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य–मलिन उपहास
तब भी कहते हो–कह डालूँ दुर्बलता अपनी बीती।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे–यह गागर रीती।
किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले–
अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले।
काव्यांश १ की व्याख्या: अस्वीकृति के तर्क
कवि अपने मन रूपी भँवरे से पूछते हैं कि वह गुनगुनाकर अपनी कौन-सी कहानी कह रहा है, जबकि जीवन रूपी वृक्ष की सुखद पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं। कवि मानते हैं कि इस विस्तृत संसार में असंख्य महान व्यक्तियों का जीवन इतिहास मौजूद है, जिसे पढ़कर लोग केवल उनका उपहास (मजाक) ही करते हैं।
कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या वे उनकी दुर्बलताओं (कमजोरियों) की कथा सुनकर सुख प्राप्त करेंगे? उनका जीवन तो उस ‘गागर रीती’ (खाली घड़े) के समान है, जिसमें सुख का कोई रस नहीं है। कवि चेतावनी देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दें, जिसे पढ़कर मित्र स्वयं को ‘खाली करने वाला’ समझ लें—यानी यह न मान लें कि उन्होंने ही कवि के जीवन से सुख का रस छीनकर उनका जीवन दुखों से भर दिया। यह तर्क कवि के आत्म-सम्मान को दर्शाता है और आत्मकथा न लिखने का एक शालीन कारण प्रस्तुत करता है।
काव्यांश २
यह विडंबना! अरी सरलते तेरी हँसी उड़ाऊँ मैं।
भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊँ मैं।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ, मधुर चाँदनी रातों की।
अरे खिल–खिला कर हँसते होने वाली उन बातों की।
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया।
आलिंगन में आते–आते मुसक्या कर जो भाग गया।
काव्यांश २ की व्याख्या: निजीता की रक्षा
कवि अपने सरल स्वभाव पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह बड़े दुर्भाग्य (विडंबना) की बात होगी यदि वे अपने सरल स्वभाव की हँसी उड़ाएँ। वे नहीं चाहते कि आत्मकथा लिखकर वे अपनी भूले (गलतियाँ) या दूसरों के दिए हुए धोखे (प्रवंचना) दुनिया के सामने लाएँ, जिससे उन धोखेबाज मित्रों को शर्मिंदा होना पड़े।
कवि अपनी पत्नी के साथ चांदनी रातों में बिताए हँसने-बोलने के मधुर, एकांत क्षणों को ‘उज्ज्वल गाथा’ कहते हैं और उन्हें सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये क्षण उनके सबसे पवित्र और निजी हैं। कवि अत्यंत दुख के साथ कहते हैं कि जिस सुख का उन्होंने स्वप्न देखा था, वह उन्हें कभी मिला ही नहीं। सुख उनकी बाहों में आते-आते (यानी पत्नी की मृत्यु से पहले ही) मुस्कुराकर भाग गया। उनकी सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना पत्नी की अकाल मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई और उनका जीवन दुखों से भर गया।
काव्यांश ३
जिसके अरुण–कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में।
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में।
उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की।
सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की?
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ?
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ?
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म–कथा?
अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।
काव्यांश ३ की व्याख्या: मौन की महत्ता
कवि अपनी प्रिया (पत्नी) के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गालों की मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया से ही प्रेम बिखेरती हुई ‘अनुरागिनी उषा’ (प्रेमपूर्ण सुबह) अपनी ‘सुहाग मधुमाया’ (लाल रंग/सौंदर्य) लिया करती थी।
आज उन्हीं प्रिय स्मृतियों का सहारा (पाथेय) लेकर वे अपने जीवन-पथ की थकान दूर कर रहे हैं। कवि पूछते हैं कि क्यों लोग उनकी अंतरमन रूपी गुदड़ी की सिलाई (सीवन) को उधेड़कर उसके भीतर के दुखों को देखना चाहते हैं? कवि का जीवन छोटा है, इसलिए उसमें बड़ी-बड़ी कहानियाँ सुनाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। वे कहते हैं कि यह बेहतर होगा कि वे चुप रहकर (मौन रहकर) अन्य महान लोगों की कहानियों को सुनें।
वे अंत में दृढ़ता से कहते हैं कि उनकी भोली आत्मकथा (साधारण जीवन गाथा) सुनकर भला किसी को क्या मिलेगा? इसके अलावा, अभी सही समय नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का दुःख अब थककर शांत हो गया है। कवि अपने दुखद अतीत को कुरेदकर, फिर से दुखी होने के लिए उसे जगाना नहीं चाहते हैं। यह तर्क कवि के संयम और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करता है।
III. अपनी बात
“निष्कर्ष रूप में, ‘आत्मकथ्य’ केवल एक आत्मकथा लिखने से इनकार नहीं है, बल्कि यह एक महान कवि का विनम्र आत्म-निवेदन है। जयशंकर प्रसाद ने मौन और संयम को अपनाकर, जीवन के दुखों को सार्वजनिक उपहास का विषय बनने से रोका है। यह कविता सरलता, निजीता की गरिमा, और दुख के प्रति शांत स्वीकृति का पाठ पढ़ाती है।”