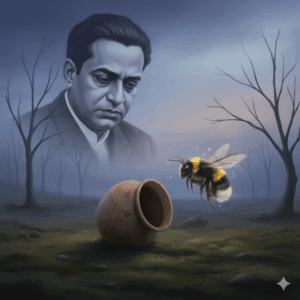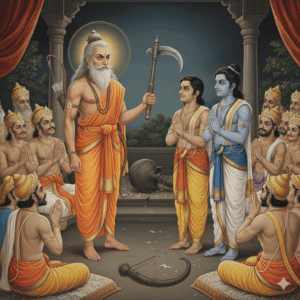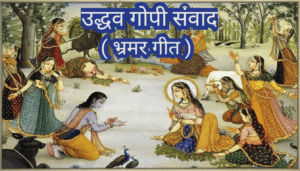I. कविता का संक्षिप्त सार
‘यह दंतुरित मुस्कान’ कविता में कवि नागार्जुन ने एक छोटे शिशु के नए-नए निकले दाँतों (दंतुरित) वाली मुस्कान की मादकता का वर्णन किया है। कवि लम्बे समय बाद घर लौटते हैं और पहली बार अपने शिशु को देखते हैं। शिशु की यह भोली मुस्कान कवि के कठोर और उदासीन मन को भी पिघला देती है।
कवि कहते हैं कि शिशु की इस मुस्कान में इतनी शक्ति है कि यह मृतक में भी प्राण डाल सकती है, पत्थर को भी जल बना सकती है, और बाँस या बबूल जैसे कठोर पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़वा सकती है। शिशु की दृष्टि पहले कवि को अपरिचित मानकर देखती है, लेकिन जब माँ दोनों के बीच सेतु (मध्यस्थ) का काम करती है, तो शिशु अपने पिता को पहचानकर मुस्कुरा देता है।
कवि मानते हैं कि इस मधुर मुस्कान के दर्शन से उनका जीवन धन्य हो गया है। कवि शिशु की माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिसने इस मुस्कान को कवि तक पहुँचाया। यह कविता माँ और बच्चे के संबंधों, शिशु-सौंदर्य और वात्सल्य रस का अद्भुत उदाहरण है।
II. विस्तृत व्याख्या (काव्यांशों के आधार पर)
काव्यांश १: मुस्कान की अद्भुत शक्ति
तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान
मृतक में भी डाल देगी जान।
धूलि धूसर तुम्हारे ये गात…
छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात।
परस पाकर तुम्हारा ही प्राण
पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े
शेफालिका के फूल—
बाँस था कि बबूल?
व्याख्या: कवि शिशु की नए-नए निकले दाँतों वाली मुस्कान को देखते हैं और कहते हैं कि यह इतनी अद्भुत है कि इसमें मृतक में भी जान डालने की शक्ति है। अर्थात्, यह मुस्कान निराश और हताश व्यक्ति को भी जीवन की ओर प्रेरित कर सकती है।
कवि शिशु के धूल-मिट्टी से सने हुए शरीर (धूलि धूसर तुम्हारे ये गात) को देखते हैं, और उन्हें यह मिट्टी सना शरीर इतना प्रिय लगता है कि उन्हें भ्रम होता है कि मानो तालाब को छोड़कर कमल (जलजात) उनकी झोंपड़ी में खिल उठे हों।
कवि आगे कहते हैं कि शिशु का स्पर्श (परस) पाकर तो कठिन पत्थर (कठिन पाषाण) भी पिघलकर जल बन गया होगा। यह मुस्कान इतनी जादुई है कि यदि कोई बाँस या बबूल (जो कठोरता और नीरसता के प्रतीक हैं) भी शिशु को छू ले, तो उससे भी शेफालिका (सुगंधित फूल) के कोमल फूल झरने लगेंगे। इस प्रकार, कवि शिशु की मुस्कान की अपरिमित सकारात्मक शक्ति का वर्णन करते हैं।
काव्यांश २: पिता और शिशु का संवाद
तुम मुझे पाए नहीं पहचान?
देखते ही रहोगे अनिमेष!
थक गए हो?
आँख लूँ मैं फेर?
क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार?
यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज
मैं न देख पाता
मैं न जान पाता
तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान।
व्याख्या: लम्बे समय बाद लौटे कवि अपने शिशु से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? शिशु कवि को बिना पलक झपकाए (अनिमेष) लगातार देख रहा है, क्योंकि कवि उसके लिए अपरिचित हैं। कवि बालक के प्रति स्नेह और चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मुझे देखते-देखते थक गए हो? यदि ऐसा है, तो मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ ताकि तुम्हें लगातार देखना न पड़े।
कवि स्वीकार करते हैं कि यदि हम पहली बार परिचित नहीं हो पाए तो क्या हुआ? यह स्वाभाविक है। कवि अपनी पत्नी (माँ) के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम (सेतु या जोड़ने वाली कड़ी) न बनी होती, तो मैं तुम्हारी इस मोहक मुस्कान को न तो देख पाता और न ही इसकी अद्भुत शक्ति को जान पाता। यहाँ माँ का माध्यम बनना यह बताता है कि माँ के कारण ही पिता और पुत्र के बीच स्नेह का संबंध स्थापित हो पाया है।
काव्यांश ३: शिशु के प्रति वात्सल्य
धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य!
चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य!
इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क?
उँगलियाँ फेरती रही है माँ
मधुपर्क।
देखते तुम इधर कनखी मार
और होती जबकि आँखें चार
तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान
मुझे लगती है बड़ी ही छविमान!
व्याख्या: कवि शिशु की मुस्कान के दर्शन से अभिभूत होकर शिशु को और उसकी माँ दोनों को धन्य कहते हैं। कवि स्वयं को ‘चिर प्रवासी’ (लंबे समय तक बाहर रहने वाला) और ‘इतर’ (दूसरा), ‘अन्य’ (अजनबी) मानते हैं, जिसका शिशु से कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। कवि शिशु से पूछते हैं कि अतिथि जैसे मुझ (पिता) से तुम्हारा क्या संपर्क रहा होगा? शिशु को माँ ही पालती हैं। माँ अपनी उँगलियों से शिशु को प्रेमपूर्वक ‘मधुपर्क’ (दही, घी, शहद आदि का मिश्रण, यहाँ प्रेमपूर्ण भोजन का प्रतीक) खिलाती रही है।
अंत में, कवि कहते हैं कि जब शिशु तिरछी नजरों से (कनखी मार) उनकी ओर देखता है और जब उन दोनों की आँखें मिलती हैं (आँखें चार होती हैं), तो शिशु अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेर देता है। शिशु की वह मुस्कान कवि को अत्यंत मनमोहक (बड़ी ही छविमान) लगती है। यह मुस्कान कवि के जीवन में वात्सल्य और प्रेम का संचार करती है।
निष्कर्ष: ‘यह दंतुरित मुस्कान’ का अंतिम संदेश
‘यह दंतुरित मुस्कान’ कविता में नागार्जुन ने शिशु-सौंदर्य और वात्सल्य रस को अत्यंत मार्मिकता से उकेरा है। यह कविता केवल एक शिशु की मोहक मुस्कान का वर्णन नहीं करती, बल्कि उस मुस्कान की (परिवर्तनकारी) शक्ति को भी दर्शाती है, जो एक उदासीन और कठोर मन वाले व्यक्ति में भी प्रेम, खुशी और जीवन का संचार कर सकती है। कवि ने माँ के महत्व को भी रेखांकित किया है, जो पिता और पुत्र के बीच सेतु का काम करती है। यह कविता हमें जीवन की निराशाओं के बीच छोटे-छोटे, निश्छल आनंदों के मूल्य को पहचानने और उनसे प्रेरणा लेने का संदेश देती है।