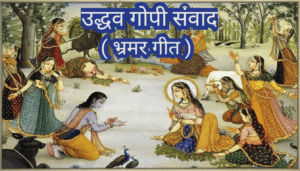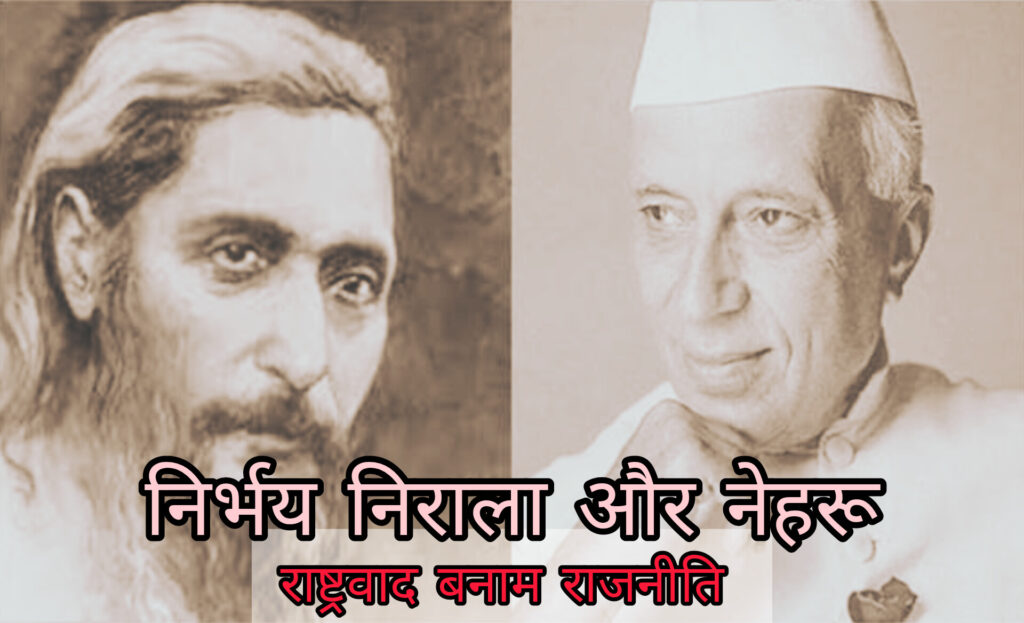
कई कार्यक्रमों में अथवा लोगों से सुना है कि निराला और नेहरू हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े दो प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिनका रिश्ता विचारों के आदान-प्रदान और कभी-कभी मतभेद का भी था। पंडित नेहरू ने सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए साहित्य अकादमी से मदद की और उनके लिए मासिक वृत्ति की व्यवस्था की। इसके अलावा, दोनों के बीच हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर भी बहस हुई थी, जिसमें निराला ने हिंदी के स्वाभिमान की रक्षा की। क्या आपको नहीं लगता कि इस वाक्य में चाटुकारिता और चापलूसी की नैतिक खुशबू आ रही है। रही बात निराला की तो हिंदी की बात ही छोड़ें अगर किसी भी भारतीय भाषा का जानकार होगा वो उन्हें भली भांति जानता होगा। वो हिंदी के महाकवि थे, हैं और रहेंगे भी, किन्तु नेहरू साहित्यकार तो रहने ही दीजिए वो राष्ट्रवादी भी नहीं थे, अगर वो कुछ थे सिर्फ राजनैतिक विचारधारा के अनुयाई। और वो भी ऐसे अनुयाई जो सिर्फ गांधी से थे या गद्दी से यह तो पता नहीं, मगर गांधी के ओट में हमेशा रहे।
गांधी का हिंदी प्रेम…
ये वो ही गांधी हैं, जिनसे हिंदी की अस्मिता को लेकर निराला की भिड़ंत हो गई थी, और निराला जी ने अपनी खिन्नता को इतना विस्तार से लिखा कि बापू के आलोचक आजतक इसका इस्तेमाल करते हैं।
बात यह थी कि गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में एक वक्तव्य दिया कि ‘हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हिंदी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिंदी बोलने वालों में रवीन्द्रनाथ कहां हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहां हैं? जगदीश बोस कहां हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा मात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है, उसमें ऐसे महान व्यक्तियों के होने की आशा रखी ही जायेगी।” इस पर निराला जी भड़क गए और उन्होंने गांधीजी से मिलकर अपनी बात रखी, “आपके सभापति के अभिभाषण में हिंदी के साहित्य और साहित्यिकों के संबंध में, जहां तक मुझे स्मरण है, आपने एकाधिक बार पं बनारसीदास चतुर्वेदी का नाम सिर्फ़ लिया है। इसका हिंदी के साहित्यिकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने सोचा था? आपको क्या अधिकार है कि आप कहें कि हिंदी में रवींद्रनाथ ठाकुर कौन हैं?” आगे कुछ और बातें निराला कहते गांधी यह कह कर चले गए मेरे पास इसके लिए समय नहीं है।
निराला जी ने इसपर लिखा है कि मैं हैरान होकर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति को देखता रहा, जो राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को रास्ता बतलाता है, बेमतलब पहरों तकली चलाता है, प्रार्थना में मुर्दे गाने सुनता है, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति है, लेकिन हिंदी के कवि को आधा घंटा वक्त नहीं देता- अपरिणामदर्शी की तरह जो जी में आता है, खुली सभा में कह जाता है, सामने बगलें झांकता है!’’
नेहरू से पहली मुलाकात…
कुछ बातें यह भी सुनने या पढ़ने में आती हैं कि जवाहरलाल नेहरू और निराला दोनों के बीच इलाहाबाद में एक सभा के दौरान मुलाकात हुई थी, मगर यह भी सच नहीं है क्योंकि दोनों के से मिलने का ब्यौरा बेहद दिलचस्प है।
निराला लखनऊ से देहरा एक्सप्रेस ट्रेन से अयोध्या जा रहे थे। उनके पास इंटर क्लास का टिकट था। उसी ट्रेन में संयोगवश नेहरू भी थे। जुगत·जुगाड़ लगा कर निराला नेहरू जी के डब्बे में चले आए। उस समय नेहरू दरवाजे पर खड़े हो कर अपने साथियों से मिल-जुल रहे थे और निराला भीतर आकर उसी बर्थ पर बैठ गए, जो नेहरू के लिए नियत थी। ठीक सामने की बर्थ पर नेहरू के बहनोई आर एस पंडित बैठे थे, जिनसे निराला ने अपना औचित्य बताया कि पहाड़ मेरे पास नहीं आता तो मैं पहाड़ के पास जाऊंगा। जब नेहरू आकर अपने बर्थ पर बैठे तब निराला ने उनसे कहा – ‘आपसे कुछ बात करने की गरज से अपनी जगह से यहां आया हुआ हूं।’ इस बात को हम निराला की बोली में ही यहां उद्धृत करते हैं –
“पंडित जी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा। मुझे मालूम दिया, निगाह में प्रश्न है- तुम कौन हो? मालूम कर, अखबारों में और हिन्दी के इतिहासों में आई तारीफ का उल्लेख नाम के साथ करते हुए मैंने कहा,‘यह सिर्फ थोड़ी- सी जानकारी के लिए कह रहा हूं। प्रसिद्धि के विचार से आप खुद समझेंगे कि मैं जानता हूं कि मैं किनसे बात कर रहा हूं।’ आगे क्या हुआ क्या बातें हुईं यह हम आगे देखेंगे, मगर इतना तो साफ है कि निराला और नेहरू इस यात्रा से पहले कहीं नहीं मिले थे और ना एक दूसरे से परिचित थे।
हिंदी पर राजनीति…
रेडियो के शुरुआती दौर में रेडियो पर उर्दू का दबदबा हुआ करता था, मगर जनमानस को बहकावे में रखने के लिए उसे हिंदुस्तानी का नाम दिया जाता था, जिससे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों ने ऑल इंडिया रेडियो का साइलेंटली बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। हिंदी साहित्यकारों को अपनी भाषा के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार से बेहद निराशा थी और वे रेडियो में जाने से बचते थे। निराला ने भी इस बहिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा के प्रति गहरा सम्मान था।
प्रख्यात हिंदी सेवी पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी की अप्रत्यक्ष अगुवाई में यह सवाल उठाया गया कि रेडियो पर हिंदी का कोई कार्यक्रम क्यों प्रसारित नहीं होता? प्रख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा, ‘माधुरी’ पत्रिका के संपादक पंडित रूप नारायण पाण्डेय, उपन्यासकार यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकार उनके साथ थे और निराला तो थे ही हिंदीसेवी। यह विरोध अथवा बहिष्कार इतना प्रबल था कि भारतीय राजनीति के दो बाहुबली गांधी और नेहरू को अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आई, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। वैसे तो गांधी पहले से ही अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने नेहरू को भी हिंदी साहित्य में रुचि लेने को कहा। इसके पीछे कारण यह था कि जवाहरलाल नेहरू एक धनी रसूखदार वकील परिवार में पैदा हुए थे और उनकी शिक्षा-दीक्षा विलायत में हुई थी। उन्होंने अपने इतिहास संबंधित साक्षात्कार को दो जिल्दों ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री‘ और ‘डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया‘ में लिखा था। उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के पास लिखी चिट्ठियों का एक संकलन ‘फादर’स लेटर टू हिज डॉटर‘ भी है जो अपने तरह की एक किताब है। इसके अलावा उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, जो उनके मानने वालों की नजर में उनके समय की राजनीति और वैचारिकता का जीवंत दस्तावेज है। इन सबका लेखन उन्होंने अंग्रेजी में किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वो भी एक साहित्यकार और इतिहासकार दोनों हैं, परन्तु जनमानस के लिए फिर भी वो कुछ नहीं थे।
यही बात गांधी पहले ही समझ चुके थे, अतः उन्होंने हिंदी भाषी और उसके साहित्यकारों को अंधेरे में रखने के लिए और हिंदी के अल्पज्ञानी की सहायता के लिए एक नई भाषा हिंदुस्तानी को रेडियो सहित अन्य माध्यमों से प्रचारित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभाओं में स्वयं को हिंदी का पूजक और रवीन्द्रनाथ ठाकुर सहित प्रफुल्लचन्द्र राय को देश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार घोषित करना शुरू कर दिया, परन्तु नेहरू को हमेशा छुपाते रहे क्योंकि रवीन्द्रनाथ और प्रफुलचंद्र राय गांधी के नजदीक तो थे, पर उनमें राजनैतिक महत्वकांक्षा नहीं थी, वो सही मायनों में साहित्यकार थे, परन्तु हिंदी में उनका हाथ तंग था। इसीलिए गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में एक वक्तव्य दिया कि ‘इस मौके पर अपने दुख की भी कुछ कहानी कह दूं। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिंदी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिंदी बोलने वालों में रवीन्द्रनाथ कहां हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहां हैं? जगदीश बोस कहां हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा मात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है, उसमें ऐसे महान व्यक्तियों के होने की आशा रखी ही जायेगी।” मेरा मानना यह है कि गांधी का यह भाषण सब कुछ कह रहा है।
आप यहां देख पा रहे हैं कि किस तरह गांधी ने नेहरू का नाम ना लेकर उन्हें साफ बचा लिया और दूसरी तरफ हिंदी के साहित्यकारों को भी हंसिए पर रख दिया। हिंदी साहित्यकारों को हंसिए पर रखने का एक फायदा यह भी मिला कि नेहरू को हिंदी साहित्यकारों में से स्थान दिलाने के लिए समय मिल गया और जनमानस को यह संदेश गया कि नेहरू भी हिंदी सेवी हैं। अंग्रेज नेहरू को पंडित नेहरू के रूप में स्थापित करने के लिए गांधी द्वारा प्रचार शुरू हो गया। इस प्रचार का प्रभाव इतना बड़ा था कि निराला जैसे महापंडित भी झांसे में आ गए और जुगत निकाल कर वह देहरा एक्सप्रेस ट्रेन में जिसमें नेहरू सफर कर रहे थे, उनके डब्बे में घुस आए। जैसा कि हमने ऊपर ही लिखा है कि नेहरू उन्हें नहीं पहचानते थे। इस पर निराला ने स्वयं अपने लेख में लिखा है–
“पंडित जी ने सिर्फ मेरी तरफ देखा। मुझे मालूम दिया, निगाह में प्रश्न है -तुम कौन हो ? मालूम कर, अख़बारों में और हिन्दी के इतिहासों में आई तारीफ का उल्लेख नाम के साथ करते हुए मैंने कहा, ‘यह सिर्फ थोड़ी -सी जानकारी के लिए कह रहा हूं।प्रसिद्धि के विचार से आप खुद समझेंगे कि मैं जानता हूं कि मैं किनसे बात कर रहा हूं।’
पंडित जी मेरी बात से जैसे बहुत खुश हुए। मैंने कहा ‘इधर हिंदुस्तानी के सम्बन्ध में आपके विचार देख कर आपसे बात करने की इच्छा हुई। आप उच्च शिक्षित हैं। हर तरह की शिक्षा की परिणति उच्चता है, न कि साधारणता। आपका देशव्यापी और विश्वव्यापी बड़प्पन भी उच्चता ही है। ज़बान जब अपने भावों के व्यक्तीकरण में समर्थ से समर्थ होती चलती है, तब वह साधारण-से साधारण हो या न हो उच्च से उच्च जरूर होती है। भाषा जन्य बहुत सी कठिनाइयां सामने आती हैं जो हिंदुस्तानी जबान को मद्दे नजर रखते हुए दूर नहीं की जा सकतीं …”
नेहरू द्वारा हिंदी को क्लिष्ट कहना…
नेहरू ने अपनी आत्मकथा में एक जगह बनारस की अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है, “बनारस की इस यात्रा के अवसर पर मुझे हिंदी साहित्य की एक छोटी-सी संस्था की ओर से मानपत्र दिया गया और वहां उसके सदस्यों से दिलचस्प बातचीत करने का अवसर मिला। मैंने उनसे कहा जिस विषय का मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है उस पर उसके विशेषज्ञों से बोलते हुए मुझे झिझक होती है; लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोड़ी-सी सूचनाएं दीं। आजकल हिन्दी में जो क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा इस्तेमाल की जाती है, उसकी मैंने कुछ कड़ी आलोचना की। उसमें कठिन, बनावटी और पुराने शैली के संस्कृत शब्दों की भरमार रहती है। मैंने यह कहने का साहस भी किया कि यह थोड़े -से लोगों के काम में आने वाली दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए और हिंदी लेखकों को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जिसे लोग समझ सकें। आम जनता के संसर्ग से भाषा में नया जीवन और वास्तविक सच्चापन आ जाएगा। इससे स्वयं लेखकों को जनता की भाव -व्यंजना शक्ति मिलेगी और वे अधिक अच्छा लिख सकेंगे। साथ ही मैंने यह भी कहा कि हिन्दी के लेखक पश्चिमी विचारों या साहित्य का अध्ययन करें तो उससे उन्हें बड़ा लाभ होगा। यह और भी अच्छा होगा कि यूरोप की भाषाओं के साहित्य और नवीन विचारों के ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कर डाला जाए। मैंने यह भी कहा कि आज गुजराती, बंगला और मराठी साहित्य इन बातों में हिन्दी से अधिक उन्नत हैं; और यह तो मानी हुई बात है कि पिछले वर्षों में हिन्दी की अपेक्षा बंगला में कहीं अधिक रचनात्मक साहित्य लिखा गया है।”
नेहरू के बनारस वाले वक्तव्य पर महीनों हिन्दी अखबारों और पत्रिकाओं में बहस होती रही। संगोष्ठी के आयोजन कर इस पर चर्चा भी की गई। निराला और उनके जैसे अनेकानेक विद्वानों ने नेहरू को हिंदी साहित्य के अध्ययन पर जोर दिया, जिसका असर यह हुआ कि नेहरू आत्मग्लानि की जगह अपने अहम में आकर अपनी बात को विस्तार देते हैं–
“यह घटना मेरे लिए आंख खोलने वाली थी। उसने बतलाया कि हिन्दी के साहित्यिक और पत्रकार कितने ज्यादा तुनुक मिजाज हैं। मुझे पता लगा कि वे अपने शुभचिंतक मित्र की सद्भावनापूर्ण आलोचना भी सुनने को तैयार नहीं थे। साफ़ ही यह मालूम होता है कि इस सबकी तह में अपने को छोटा समझने की भावना ही काम कर रही थी। आत्मा लोचना की हिन्दी में पूरी कमी है और आलोचना का स्टैण्डर्ड बहुत ही नीचा है। एक लेखक और उसके आलोचक के बीच एक दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौच होना हिन्दी में कोई असाधारण बात नहीं है। यहां का सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और दरबारी-सा है और ऐसा मालूम होता है मानो हिन्दी का लेखक और पत्रकार एक दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटे से दायरे के लिए लिखते हों। उन्हें आमजनता और उसके हितों से मानो कोई सरोकार ही नहीं है।”
निराला के सवाल…
निराला उन दिनों हिंदी और हिंदुस्तानी के सवाल पर उठे विवाद पर नेहरू को अपना नजरिया बता रहे थे, जबकि नेहरू को यह नागवार गुजर रहा था, वो यह नहीं जानते थे कि निराला हिंदी के अलावा बंगला, अंग्रेजी, रूसी साहित्य सहित अन्य भाषाओं पर भी अपनी पकड़ रखते थे। महापंडित तो फक्कड़ थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नेहरू उनसे बात करने में असहज महसूस कर रहे हैं। वो अपनी प्रवाह में बोलते हुए नेहरू के आत्मकथा के उस अंश पर आते हैं, जिसमें नेहरू ने हिंदी लेखकों को खरी-खोटी सुनाई थी। निराला पूरे आवेग से हिन्दी साहित्य की वर्तमान स्थिति का एक खाका देते हैं। उन्होंने नेहरू के सामने यह अफ़सोस जाहिर किया कि प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद के निधन पर कांग्रेस ने अपने सालाना जलसे में एक शोक प्रस्ताव तक स्वीकृत नहीं किया। इस पर नेहरू इतना ही बोल पाए कि ‘जहां तक मुझे स्मरण है प्रेमचंद जी पर तो एक शोक प्रस्ताव पास किया गया था।’ निराला ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन उसकी वैसी महत्ता नहीं, जैसी शरतचंद्र वाले की है।” इतना कह निराला ने मुलाकात के ब्योरे का समापन किया।
कालांतर में नेहरू ने इस मुलाकात को हेकड़ी का नाम दिया। उन्होंने इसे अपने लेख के माध्यम से हिन्दी रचनाकारों के आत्मसम्मान की लड़ाई की जगह हीनता कहा है।
अपनी बात…
निराला कवि हैं, लेखक हैं यह तो उस समय सभी को पता था लेकिन वो चिंतक भी हैं यह बात हिंदी और हिंदुस्तानी पर निराला के वैचारिक लेखन से पता चला। निराला के चिंतन का दायरा विस्तृत है। वे मनुष्य, समाज, राजनीति की वस्तुस्थिति और गति पर गहरी नजर रखते हैं और उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं। साथ ही, मनुष्य, समाज, राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, निराला इसे अपने चिंतन के दायरे में लाते हैं, उस पर लेखनी चलाते हैं।
उनपर छींटाकशी करने और तुनकमिजाजी के साथ हेकड़ी करने की तोहमत लगाकर नेहरू ने अपनी औपनिवेशिक विचाधारा का परिचय दिया। जबकि निराला औपनिवेशिक शासन के खिलाफ चल रही राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक और समर्थ कवि थे। निराला जहां औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना करते हैं, वहीं वह राष्ट्रीय आंदोलन और उसके नेतृत्व पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। मिसाल के तौर पर, नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो एक बार इलाहाबाद आए तो उन्होंने निराला से मिलने के लिए संदेश भिजवाया, लेकिन निराला उनसे मिलने नहीं गए। निराला ने उस समय कहा कि भाई जवाहर बुलाए तो वे नंगे पांव मिलने जा सकते है पर प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने वे नहीं जाएंगे। यह निराला के घमंड का नहीं, उनकी चैतन्य अवस्था का परिचय है। वो शक्ति और सीमा दोनों को जांचते-परखते हैं, और फिर अंतर्विरोधों को व्यक्त करते हैं। निराला अपनी सहमति और असहमति दोनों को निर्भय होकर प्रकट करते हैं।
उनकी निर्भयता ही थी कि उन्होंने गणमान्य व्यक्तित्वों पर भी अपनी लेखनी चलाई। इसी क्रम में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को केंद्रित कर लेखन किया। निराला ने नेहरू पर कविताएं भी लिखी। नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण में कितनी भूमिका रही है, यह शोध का विषय है, परन्तु गांधी के योगदान और प्रचार से नेहरू पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने में पूरी तरह से सफल हुए। चैतन्य निराला भी नेहरू से कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस प्रभाव के बावजूद राष्ट्र निर्माण से जुड़े कई सवालों पर निराला ने नेहरू की आलोचना की है।