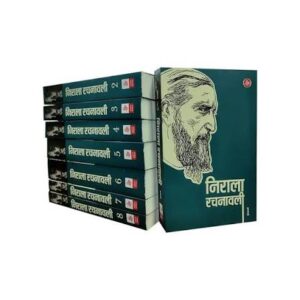भारतीय प्राच्यविद्या को अंधविश्वासों से जोड़ दिया गया, जबकि उसमें गणित, व्याकरण, काव्य, चिकित्सा की अद्भुत दृष्टियां हैं. आज कोई हिंदुस्तान की किसी बड़ी अकादमी से पढ़कर निकले और राजशेखर, भरतमुनि, व्यास, पाणिनि, आर्यभट या कुमारिल को उद्धृत करे! इस पूरी ज्ञान-परंपरा को ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहकर निरस्त करने की कोशिशें आज भी की जा रही हैं!
संस्कृत का नाम लो तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नाक-भौं सिकोड़ते हैं और “अष्टाध्यायी” और “अमरकोश” की बात करो तो सामान्यजन यूं कौतुक से देखते हैं, जैसे किन्हीं विलायती ग्रंथों का नाम ले लिया हो! यह भारत है, जहां अच्छी अंग्रेज़ी लिखना गर्व की बात मानी जाती है और अच्छी हिंदी हमें असहज कर देती है. सुशोभित को तो उसकी क्लिष्ट तत्समनिष्ठ हिंदी के लिए तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नियमित टोका जाता है तो किसी और की बात क्या करें! योग तक को “भगवा” माना जाता है!
हमारे बुद्धिजीवी रात-दिन भारतीय परंपरा को कोसते रहते हैं. अवैज्ञानिक कहते हैं. गीता, उपनिषद, योग उपहास्य हैं. ज्योतिष अंधविश्वास है. आयुर्वेद तिथिबाह्य है. फिर व्याकरण और काव्य सिद्धांत की तो बात ही क्यों करें? षट्दर्शन की चर्चा फिर कौन करे? दुनिया के उत्तर आधुनिक चिंतक नागार्जुनाचार्य से फ़िलॉस्फ़ी सीखते हैं और पाणिनी से व्याकरण सीखते हैं पश्चिम के भाषाचिंतक! और हम इनके दाय से भी अनभिज्ञ! पाणिनी के पारिभाषिक शब्द जो सर्वज्ञात होने चाहिए थे, आज हमारे लिए कौतुक और आश्चर्य का विषय हैं. और कश्मीर को भी हम आज राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों से ही जानते हैं, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कल्हण और क्षेमेन्द्र के देश के रूप में नहीं. यह हमारी शिक्षा परंपरा पर ही एक टिप्पणी है
आत्मघृणा, आत्म-धिक्कार और आत्मग्लानि
औपनिवेशिक हीनता-बोध से उपजे रीढ़हीन आत्म-दैन्य को उन्होंने अपने चिंतन का व्याकरण बना लिया. हर हिंदू प्रतीक घृणित हो गया, चाहे वह कितना ही उदात्त क्यों ना हो. हर हिंदू रूपक लज्जास्पद हो गया, चाहे वह कितना ही निरापद क्यों ना हो. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जातीय अस्मिता से जोड़ा जाने लगा. और इसमें दक्षिणपंथ और वामपंथ की एक भीषण दुरभिसंधि को भी आप लक्ष्य कर सकते हैं. दक्षिणपंथ कहता है : “उग्र राष्ट्रवाद ही हिंदुत्व है.” वामपंथ कहता है : “जी हां, और इसीलिए हिंदू अस्मिता एक त्याज्य मूल्य है.” यह एक श्रेष्ठ और सहिष्णु सांस्कृतिक परंपरा पर दोहरा प्रहार है : भीतर से और बाहर से!
बहुत याद आते हैं गोपीनाथ कविराज, भगवतशरण उपाध्याय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद वात्स्यायन, विद्यानिवास मिश्र, श्रीनरेश मेहता और निर्मल वर्मा : इन मनीषियों के होते “हिंदू-भर्त्सना” का ऐसा सामूहिक एकालाप संभव ना होने पाता, जैसा कि आज
कोई भी जाति आठों पहर आत्मग्लानि में डूबी नहीं रह सकती. गौरव जातीय अस्मिता का ग्रास है. उससे वह पुष्ट होती है. सनातन परंपरा आत्ममंथन में स्वयं सक्षम है और सुधारों के लिए तत्पर भी रही है, फिर भी उसे हमेशा लज्जित करने के प्रयास क्यों किए जाने चाहिए?
इति नमस्कारन्ते