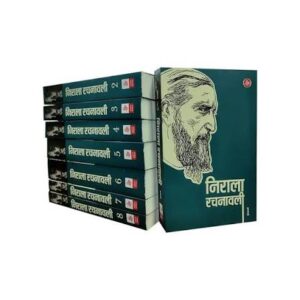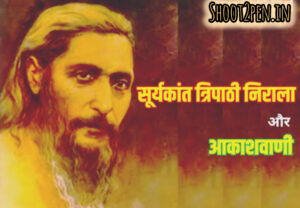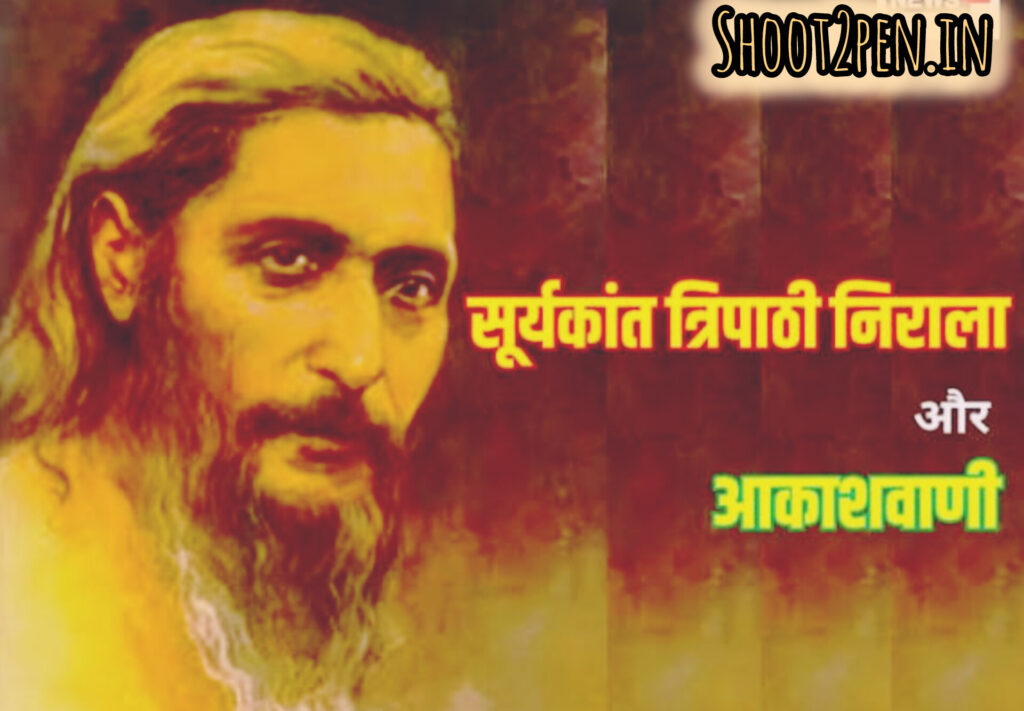
रेडियो के शुरुआती दौर में उसकी भाषा तथाकथित हिंदुस्तानी हुआ करती थी अर्थात उर्दू के शब्दों की भरमार वाली हिंदी। उस समय रेडियो पर जो कार्यक्रम होते थे उन पर पारसी थियेटरों का बहुत असर हुआ करता था। नाटकों में राम को राजकुमार की जगह शहजादा और माता सीता को बेगम कहा जाता था। तथा किसी पात्र के प्रकट होने पर ’जलवा अफरोज’ हुआ कहते थे। यह ऐसी भाषा थी जिसको लेकर हिंदी प्रेमियों के मन में गहरा असंतोष था।
निदान की कोशिश…
प्रख्यात हिंदी सेवी पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी की अप्रत्यक्ष अगुवाई में यह सवाल उठाया गया कि रेडियो पर हिंदी का कोई कार्यक्रम क्यों प्रसारित नहीं होता? प्रख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा, ‘माधुरी’ पत्रिका के संपादक पंडित रूप नारायण पाण्डेय, उपन्यासकार यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकार उनके साथ थे। इस पर यह तय हुआ कि हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। लेकिन सवाल था कि उसे करेगा कौन?
लखनऊ रेडियो के डायरेक्टर थे हसीब साहब। उन्होंने बारी-बारी से सभी साहित्यकारों से अनुरोध किया कि वे साहित्यिक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी संभालें लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन सभी ने एकमत से नाम सुझाया- पंडित बलभद्र दीक्षित ‘पढ़ीस’। पढ़ीस जी अवधी के कवि के रूप में विख्यात थे और रेडियो में प्रतिलिपिकार (कॉपिस्ट) के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें हिंदी के कार्यक्रमों का जिम्मा सौंप दिया गया।
पढ़ीस जी ने सोचा कि हिंदी का कार्यक्रम किसी बड़े लेखक या कवि के रचनापाठ से शुरू हो। उस समय हिंदी के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ उत्थान पर थे और पढ़ीस जी को मनाते भी थे। वह निराला जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप चलिए और रेडियो पर कविता पाठ कीजिए।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शुद्ध बैसवारी में कहा- ‘सरठ, हुआं सहजादा राम और बेगम सीता रौनक अफरोज होति है और हमका तुम कहत हौ कि कविता पाठ करौ। को सार सुनी हुवां हमार कविता?’ पढ़ीस जी ने हाथ जोड़ कर कहा कि पंडितजी रेडियो अब बहुतों के पास पहुंच रहा है और, सोचिए कि एक साथ लाखों लोग आपकी वाणी सुनेंगे। बहरहाल महाकवि निराला जी रेडियो पर काव्य-पाठ के लिए राजी हो गए।
कार्यक्रम का दिन…
कार्यक्रम के दिन लगभग साढ़े सात बजे निराला जी रेडियो स्टेशन पहुंच गए, जबकि कार्यक्रम रात आठ बजे प्रसारित होना था। पढ़ीस जी कार्यक्रम की उद्घोषणा लिखने के लिए निराला जी से बातें करने लगे कि वह कौन सी कविता पढ़ेंगे, कविता का क्या शीर्षक है आदि आदि। निराला जी ‘राम की शक्तिपूजा’ का पाठ करने वाले थे। पढ़ीस जी ने सोचा कि हिंदी का पहला कार्यक्रम है, जरा ओजपूर्ण ढंग से उसकी शुरूआत हो, तो ‘राम की शक्तिपूजा’ से ज्यादा ओजपूर्ण और क्या हो सकता था।
रेडियो में एक उद्घोषक थे महाशय अयाज साहब। वह रेडियो के निदेशक जेड. ए. बुखारी की आंखों के तारे थे। उन्होंने देखा कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो उसकी उद्घोषणा तो उन्हीं को करनी चाहिए। अयाज साहब ने पढ़ीस जी से कहा ‘पंडित जी यह उद्घोषणा तो मैं ही करूंगा।’ पढ़ीस जी हक्के-बक्के से रह गए। बुखारी साहब की वजह से अयाज साहब की बात रेडियो स्टेशन में कोई टाल नहीं पाता था। पढ़ीस जी ने कहा- ‘ठीक है, आप चाहते हैं तो आप ही कीजिए उद्घोषणा।’
निराला जी को स्टूडियो ले जाया गया। ड्यूटी रूम में ड्यूटी ऑफिसर रेडियो पर कान लगा कर बैठ गया। प्रतीक्षा होने लगी कि अब कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होने वाला है।
रेडियो पर उद्घोषणा हुई अभी आप फलां ‘पिरोगराम’ सुन रहे थे और अब होगा ‘कबीता पाठ’। कबी हैं पंडित सूर्य कान्ता त्रिपाठा निराली। इसके बाद महाकवि की काव्य पाठ होनी चाहिए थी लेकिन रेडियो पर जो आवाजें सुनाई देने लगीं उसे सुन कर ड्यूटी ऑफिसर को लगा कि शायद रेडियो में कोई खराबी आ गई है। उसने ठोंक-पीट कर देखा, रेडियो तो ठीक था। वह स्टूडियो की तरफ भागा। स्टूडियो के मोखे से झांक कर देखा कि अयाज साहब की गरदन निराला जी की फौलादी बाँह में फंसी हुई है, उनके मुंह से वही घुटी-घुटी आवाजें निकल रही हैं जो रेडियो पर सुनाई दे रही थीं। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद गरदन बाँह के शिकंजे से छूट नहीं पा रही थी और महाकवि रौद्र रूप में बैठे हुए हैं।
ड्यूटी ऑफिसर यह दृश्य देख कर घबरा गया। उसने स्टूडियो कॉरीडार में लगे इंटरकॉम से तुरंत कंट्रोल रूम को फोन किया कि काट कर जल्दी से फिलर लगाइए। इस बीच हल्ला मच गया कि स्टूडियो में कुछ हो गया है। लोग आ-आ कर देखते कि अयाज साहब महाकवि की एक बाँह में कुछ इस तरह जकड़े हुए हैं, जैसे; बाली के कांख में रावण।
दरअसल उन दिनों आज की तरह शीशे की विभाजन दीवार के साथ उद्घोषक और कलाकार के लिए अलग-अलग स्टूडियो नहीं हुआ करते थे। कार्यक्रमों का प्रसारण भी सजीव हुआ करता था। उद्घोषक अगर संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा होता था तो कलाकार के पास बैठ कर उसी माइक्रोफोन से बोल देता था और अगर कविता या वार्ता की उद्घोषणा करता था तो वार्ताकार या कवि के कंधे की तरफ से अपनी गरदन जरा आगे निकाल कर उसी माइक से उद्घोषणा कर दिया करता था। इसी व्यवस्था के चलते अयाज साहब की गरदन महाकवि की एक बाँह की गिरफ्त में आ गई थी।
इधर एक स्टूडियो में यह कांड चल रहा था और उधर पढ़ीस जी किसी दूसरे स्टूडियो में अगले कार्यक्रम को रिहर्सल करवाने में व्यस्त थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर निराला जी को शांत करे। समस्या यह थी कि अयाज साहब की गरदन कैसे छूटे?
‘पंडित जी कहां हैं? पंडित जी को बुलाइए ‘ निराला ने गरज कर कहा।
पढ़ीस जी आए और स्टूडियों का दरवाजा खोल कर जैसे ही भीतर घुसे निराला जी का गुस्सा फूट पड़ा। वह उठ कर खड़े हो गए। अयाज साहब की गरदन उनके कुर्सी से उठते ही छूट गई और वह अपनी जान ले कर भाग निकले।
‘सरउ तुमसे कहा रहे कि हियां हमका कविता न पढ़वाओ। हमार नांव लेते है, कहते है सूर्या कान्ता त्रिपाठा निराली। अंदर तुम कहत हो कि लाखों लोग सुनिहै’… निराला जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था।
पढ़ीस जी ने उनसे माफी मांगी और कहा कि फिर से उद्घोषणा करा कर आपका काव्यपाठ करा देते हैं। ट्रांसमिशन एक्सटेंड हो जाएगा।
निराला जी ने जवाब दिया “न, अब हियां से चलो, सीधे चलौ हियां से।’
पढ़ीस जी ने अनुरोध किया कि स्टेशन डायरेक्टर साहब से तो मिल लीजिए, वह आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं।
“उनके पास लइ चलिहौ तो उनहूं क मारब हम’ निराला जी ने कहा और चले गए। ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि उक्त घटना के बाद निराला जी फिर कभी रेडियो नहीं गए, लेकिन यह सच नहीं है।
रेडियो पर हिन्दुस्तानी की जगह हिंदी…
रेडियो से हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित हों, इस मांग को लेकर पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने प्रयास तो बहुत किए लेकिन सरकारी सेवा में होने के कारण उनका सहयोग अप्रत्यक्ष ही रहता था। उनको बराबर लग रहा था कि सरकारी नीति न सिर्फ हिंदी को रेडियो में स्थापित होने देने में बाधक है बल्कि प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भी स्तरहीन हैं।
रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और प्रसारित कार्यक्रमों पर समीक्षा प्रकाशित करने के लिए चतुर्वेदी जी ने एक पत्रिका शुरू की जिसको नाम दिया ‘आकाशवाणी’।
इसी ‘आकाशवाणी’ पत्रिका के अंक पांच में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह लेख प्रकाशित है जिसे उन्हें रेडियो पर पढ़ने नहीं दिया गया था। उस लेख में निराला जी ने सरकार की भाषा नीति की आलोचना की थी और बताया था कि किस तरह ‘हिंदुस्तानी’ के नाम पर ‘उर्दू’ को हम पर थोपा जा रहा है और किस तरह साधारण हिंदी शब्दों को भी जबरन उर्दू शब्दों में बदल दिया जाता है। पत्रिका के अंक एक में निराला जी की कविता ‘यमुना के प्रति’ प्रकाशित है जो उन्होंने १९४१ में लखनऊ रेडियो द्वारा प्रसारित एक कवि सम्मेलन में पढ़ी थी।
पुनः रेडियो पर निराला…
१९६० में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अंतिम बार आकाशवाणी आए। इस बार स्टेशन था इलाहाबाद। निराला जी एक दिन दस-साढ़े दस बजे के आसपास रिक्शे से रेडियो स्टेशन के गेट पर उतरे। प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर स्टेशन डायरेक्टर थे। उनको खबर दी गई कि निराला जी आए हैं। वह भागे-भागे आए और महाकवि को सम्मानपूर्वक अपने कमरे में लिवा ले गए। यह वह समय था जब डायरेक्टर के कमरे में बैठने का सौभाग्य सब को नहीं मिलता था।
“गिरिजा कुमार, हम रेडियो पर कविता पढ़ब’ निराला जी ने कहा तो माथुर साहब तो जैसे आसमान से धरती पर गिरे। गिरिजा कुमार माथुर ने तुरंत प्रोग्राम सेक्रेटरी को बुलाया और अनुबंध पत्र तैयार करके लाने को कहा।
‘पंडित जी, यह एक औपचारिकता है, इस कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए-‘ माथुर साहब ने निराला जी के सामने कांट्रेक्ट रखते हुए सविनय कहा।
‘दस हजार रूपैया ल्याब’ निराला जी ने कहा तो माथुर साहब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें?
दस हजार रुपए तो अगर भारत सरकार भी चाहती तो नहीं दे सकती थी। किसी कलाकार की अधिकतम फीस एक सौ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती थी और निराला जी एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि ‘दस हजार रूपैया ल्याब और कविता पढ़व।’
सुबह से दोपहर होने को आई। ऑफिस का सारा काम-काज रूका पड़ा था। निराला जी की शर्त मानी नहीं जा सकती थी और वह कविता पाठ करने पर अड़े हुए थे और वह भी अपनी शर्तों पर।
निराला जी जब तक स्मृतिभ्रंश के शिकार हो चुके थे। कोई सोची हुई बात दिमाग में ज्यादा समय तक टिकती नहीं थी और जल्दी ही पहली बात पर कोई दूसरी बात स्थान बना लेती थी।
हुआ यूं था कि निराला जी को खबर मिली कि सुमित्रानंदन पंत अस्वस्थ हैं। वह दारागंज के अपने घर से पंत जी को देखने निकले थे। चंद्रमुखी ओझा ‘सुधा’ की बहिन चंद्रकांता त्रिपाठी रेडियो में कलाकार थीं और वह निराला जी को लेकर रेडियो आ गई थीं कि निराला जी माथुर साहब से कह देंगे तो उनकी फीस बढ़ जाएगी। रेडियो पहुंच कर निराला जी के दिमाग से चंद्रकांता त्रिपाठी की फीस बढ़वाने की बात निकल गई और रेडियो में कविता पढ़ने की बात आ गई।
शाम होने को आई। आफिस बंद होने का समय हो गया। निराला जी स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में अपनी जिद के साथ जमे कि ‘दस हजार ल्याब अउर कविता पढ़ब।’ किस की हिम्मत कि निराला जी से जाने के लिए कहता। माथुर साहब ने युक्तिभद्र दीक्षित को बुलवाया और रुआंसे हो कर कहा कि किसी तरह निराला जी को यहां से ले जाओ।
निराला जी को हथेली पर मल के तैयार की जाने वाली तंबाकू खाने का शौक था। युक्तिभद्र दीक्षित भी तंबाकू खाते थे। पहले वह निराला जी के सामने तंबाकू नहीं खाते थे लेकिन एक बार जबसे निराला जी ने उन्हें खाते पकड़ लिया था और सामने खाने को कह दिया था तब से वह उनके सामने भी तंबाकू खाने लगे थे। दीक्षित जी माथुर साहब के कमरे में घुसे।
‘अच्छा, तुम हिंयई हो?’ निराला जी ने दीक्षित जी को देखते ही पूछा।
‘जी पंडित जी।’
‘तुमसी महतारी कइसी है? निरालाजी ने पूछा।
‘महतारी क तौ तुमही कांधे पर भइंसा कुण्ड पहुंचाए आए रहयो, अब महतारी के पूछत हो।” दीक्षित जी ने याद दिलाया।
‘अच्छा चलौ, तमाखु खवाओ।’ निराला जी ने कहा।
‘हां हां, तमाखू बनाइत है। आप तो पंतजी क देखै जात‘- दीक्षित जी ने कहा।’
‘हां. पंतजी क देखै जाएक है’ – निराला जी को याद आ गया कि वह किस काम से घर से निकले थे।
दीक्षित जी ने माथुर साहब से कह कर कार पहले से तैयार करवा रखी थी। उन्होंने निराला जी को कार में बैठाया और महाकवि चले गए पंत जी को देखने।
अपनी बात…
यह आलेख वाणी आकाशवाणी नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक नवनीत मिश्र जी हैं। पुस्तक का प्रकाशन सूचना विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है।