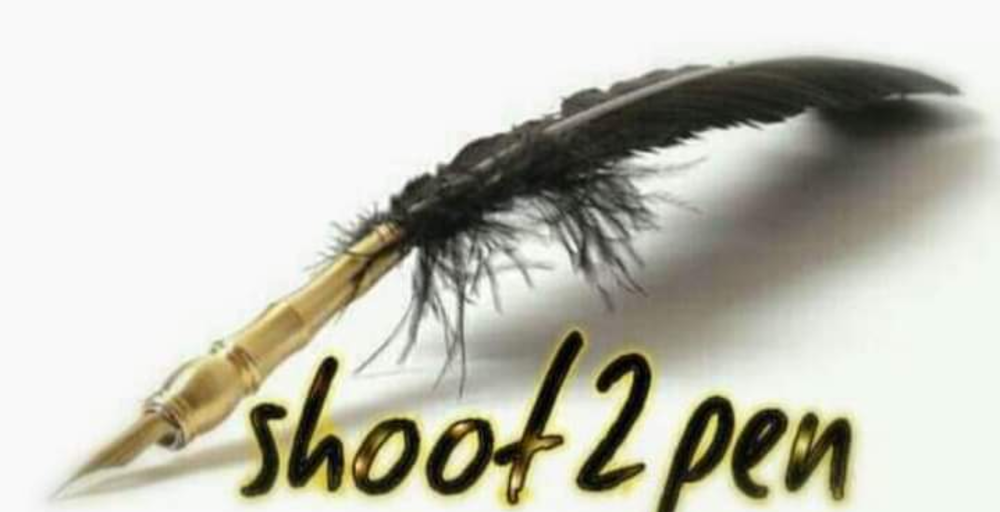
यूनानो मिश्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और जगद्गुरु श्रीकृष्ण को मानने वाले और गंगा यमुना सरस्वती के आंचल में पले, बढ़े इस भारतीय संस्कृति ने इकबाल जैसे अलगाववादी कवि पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसने भी राष्ट्रवाद को ही अपना लक्ष्य मान उसे निर्धारित कर लिया। ऐसा नहीं कि भारत में राष्ट्रवाद कोई नई बात है, जैसा कि पश्चिमी देशों के विद्वानों और भारत के वामपंथी विचाधारा के तथाकथित ज्ञानियों का मानना है, बल्कि यह तो भारत में युगों·युगों से ज्वलंत रहा है और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह अलग बात है कि आदि काल, मध्य युग और तात्कालिक राष्ट्रवाद तीनों की प्रवृत्ति अलग·अलग रही है। आदि काल में कोई विरोधी विचारधारा नहीं थी, तो राष्ट्रवाद की बात सामने आती ही नहीं थी, वह अंतःकरण में पैठी थी, नैसर्गिक थी। मध्य युग में विरोधी विचारधारा को साथ लेकर चलने पर जोर दिया जाता था, जबकि आज का राष्ट्रवाद विभिन्न धाराओं के अलगाव की बात करता है।
कुछ अच्छे कुछ बुरे पलों को, वर्ष पुरातन दिखा गया।
जाते जाते ना जाने यह, क्या कुछ हमको सिखा गया।।
आना जाना रीत यही है, पल यही अमृत विष प्याला।
आज खड़ा जो सम्मुख अपने, वह भी है जाने वाला।।
आज के समय में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर राष्ट्रवाद क्या बला है, जो आज में खोजी जानी चाहिए और वो भी पुरे विश्वास के साथ। और इससे भी जरूरी बात यह है कि इसकी खोज का आधार क्या होना चाहिए? जवाब है, जब विश्व के तमाम बड़े रचनाकार, कलमकार, विद्वान जैसे महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, भक्त सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, होमर, दाते, गेट, शेक्सपीयर, बायरन, शैली, गोर्की, चेखव, लू शुन, टॉलस्टॉय आदि के मूल्यांकन का आधार उनका साहित्य ही रहा है तो सीधी सी बात है कि आज के साहित्यकारों के मूल्यांकन का आधार भी यही होना चाहिए, यानी उनका साहित्य।
हम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की मान्यता को आधार बनाकर चलते है। आचार्य जी के अनुसार, ‘साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-संबंधों के संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाता है, जहां जगत की विभिन्न गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है।’
आज के राष्ट्रवाद को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक वह दौर, जब समाज का कोई भी वर्ग चाहे स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुस्लिम, दलित-शूद्र, अमीर-गरीब, किसान-मजदूर कोई भी क्यों न हो, सबका एक ही दुश्मन था, अंग्रेज़ी सरकार और सपना भी एक ही था, स्वराज। इसलिए उस दौर के साहित्यकार किसी भी प्रकार के विघटनकारी विचार को अपने चिंतन का आधार नहीं बना सकते थे क्योंकि उन्हें प्राचीन भारतीय परम्परा एवं सभ्यता का बराबर खयाल रहता था। वह दौर नवजागरण कालीन दौर था और नवजागरण की यह प्राथमिक शर्त होती है कि वह अपने अतीत के उन स्वर्णिम अध्यायों की खोज करता है, जिस पर उसका वर्तमान समाज गर्व कर सके। साहित्यकार के सामने औपनिवेशिक भारत और प्राचीन भारत के मध्य किसी एक को ही चुनना था। यही वजह थी कि साहित्यकारों ने प्राचीन भारत, जिसकी सभ्यता-संस्कृति मलिन हो गई थी, को पुनर्जीवित, नवनिर्मित और संरक्षित करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब कोई अपनी सभ्यता को त्याज्य मान लेता है तो उसके पास मांगी गए इतिहास की एक पोटली होती है, जिसके साथ निर्वहन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प रह ही नहीं जाता। उस समय के साहित्यकारों के समक्ष यह भी द्वंद्व का विषय था कि जागरण के बाद जो भारत बनेगा उसमें कितना प्रतिशत पुराने भारत का होगा और कितना प्रतिशत नए भारत का। इस द्वंद्व में क्रांति के स्तर पर ढेरों नायक थे और जिनपर साहित्यकारों ने अपना कलम भी चलाया था, मगर वे समय की धूल से इस तरह ढंक गए जैसे उनका कोई आस्तित्व रहा ही ना हो। इसका फायदा मिला राजनीतिक स्तर पर गाँधी व नेहरू के चश्में को। सत्ता के चाटुकार कलमकारों ने कालांतर में उसी चश्मे से देखना शुरू कर दिया और धीरे·धीरे स्वतंत्र साहित्यकारों पर भी गाँधी के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। राजनीति और साहित्य में एकरूपता नजर आने लगी, लोगों को यह दिखने लगा कि जो काम गाँधी राजनीति के माध्यम से कर रहे हैं, वही काम साहित्यकार साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं। यह कितना सच था, कितना गलत यह एक शोध का विषय है। मगर इतना तो जगजाहिर है कि पश्चिम के प्रति तात्कालिक साहित्यकारों के नजरिये पर तत्कालीन बौद्धिक चिंतन के रूप में गाँधी का सबसे गहरा प्रभाव दिखाई देता है।
आंधी में भी जलती रही गाँधी तेरी मशाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल
दे दी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल
वहीं वर्तमान साहित्यकारों के लिए, विषय के रूप में अंग्रेजी सरकार तो नहीं रही, मगर आज भी भारत की मौलिक समस्या भूख, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता आदि ही तो हैं, परंतु इसके बावजूद भी आधुनिक साहित्य ने राष्ट्रवाद को विकास करने में अहम भूमिका निभाई है। इसका श्रेय आधुनिक हिन्दी साहित्य को जाता है। वर्तमान साहित्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को लेकर छटपटाहट यहां देखी जा सकती है।
साहित्य में अभी शास्त्र और शास्त्रियों का बोलबाला है,
अभी यहां बहुत गड़बड़ घोटाला है।
साहित्य में अभी लोकतंत्र आना शेष है,
साहित्य में भी तो एक पूरा महादेश है।
आजादी पूर्व के साहित्य में भी भारतीय जनता के दुःख-दर्द को देखा जा सकता है। उस दौर में भी ये साहित्यकार इन्ही प्रमुख सवालों से टकराते रहे हैं, जो आज के समय में मौजूद असमानता, शोषण, धर्म, जाति-वर्ण व्यवस्था, गरीबी-अभाव जैसे प्रमुख समस्याएं हैं। लेकिन उस समय का टकराव पत्थर व पानी का था, मगर आज का टकराव पत्थर और लोहे का है। पानी में भी पत्थर अपने आकार को बदलता है, लेकिन यह प्रक्रिया उस प्रक्रिया से बेहद धीमी होती है। उदाहरणस्वरूप स्वाधीनता पूर्व के साहित्य में जाति व्यवस्था, शोषण, असमानता व धर्म की बात को तो शुरू से लेकर चले लेकिन उसे लेकर कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे या पहुँचे भी तो इसकी गति काफी धीमी रही। इस धीमेपन से असंतुष्ट होकर आज के साहित्यकार हृदय परिवर्तन को छोड़कर यथार्थवादी समाजवाद का सहारा लेने लगे हैं। साहित्य अब सामाजिक सक्रियता की ओर बढ़ना चाहता है। आज का समय उस दौर का साक्षी है, जहां मनुष्य के अमानवीकरण की गति में तीव्रता आई है। जबकि वैचारिक दृष्टि से समाजवाद का स्वप्न ध्वस्त हुआ है, तो यांत्रिक सभ्यता का कहर भी विद्यमान है। मानवता को खूंटियों पर टांग देने का प्रयास हो रहा हो। आज साहित्यकार को न केवल आक्रोश व्यक्त करना होता है, बल्कि वह उस विचारहीनता को चुनौती दे रहा है।
मैं समाजवाद हूं
पूंजीवाद की छाया के तले
आज मैं आबाद हूं
देखता नित दिन मैं
श्रमिक को पिसता हुआ
आम आदमी को कटता हुआ
मरता हुआ, घिसता हुआ
आजादी के इतने बड़े अंतराल के बाद भी वही हवा, वही पानी और वही रोटी की समस्या, कुछ भी तो नहीं बदला है। क्रूर तंत्र के बाद एक नया चेहरा आया है भ्रष्ट तंत्र का चेहरा, जबकि आजादी पूर्व के साहित्य में एक सपना था…
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है?
मुट्ठी में है तकदीर हमारी,
हमने किस्मत को बस में किया है।
आज के साहित्य का आक्रोश भी संयमित नहीं है, वह छीन लेना चाहता है, वह राक्षस बनने की प्रक्रिया पर है।
हुँकारों से महलों की नींव उखड़ जाती,
साँसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,
जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ ?
वह जिधर चाहती, काल उधर ही मुड़ता है।
आजादी पूर्व साहित्य में चतुर्भुज नजर आता है, कहीं आयात तो कहीं वर्ग के रूप में, जिसके चारों छोर पर अंग्रेज, दलित, स्त्री और किसान/मजदूर होते थे। आप उस समय के किसी भी कहानी को या उपन्यास को, सभी में यही दिखाई पड़ते हैं। कहीं भी बाहरी दुनिया, शासन, उन्नति, विश्व शक्ति की बात नजर ही नहीं आती। बस आमजन के दुःख-दर्द व उसकी अभिव्यक्ति प्रमुखतया से होती थी मगर राष्ट्रीयता की साफ साफ सुनाई पड़ती थी, उसकी गंध हृदय में बसती थी।
हिमाद्रि तुंग़ शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीं।
स्वय प्रभा समुज्ज्वला स्वंतंत्रता पुक़ारती॥
अमर्त्यं वीर पुत्र हो, दृढ- प्रतिज्ञ सोंच लो।
प्रशस्त पुण्यं पंथ हैं, बढे चलों, बढे चलो॥
राष्ट्रीयता अन्य विषयों में साहित्य रचना का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, परंतु आज की रचना में राष्ट्रीयता को एक संकीर्ण एवं पिछड़ेपन वाली मानसिकता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, विशेषकर उन पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों एवम वामपंथियों द्वारा, जो औपनिवेशिक दासता को पीठ पर लादकर बेहद प्रसन्न हैं, उन्हें इसके अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता।
हाथ जो चट्टान को
तोडे़ नहीं, वह टूट जाये,
लोहे के सौ तार को
मोड़े नहीं, वह टूट जाये।
वहीं राष्ट्रवादियों ने अपने साहित्य के माध्यम से देश के स्वरूप का मनोरम चित्र उपस्थित किया, उसकी महिमा का गायन किया। अनेक रचनाओं में भारत के अतीत पर जहां गौरव दिखता है वहीं वर्तमान स्थिति की दुरावस्था का मार्मिक चित्र भी प्रस्तुत किया है। उनकी कविताओं में चुनौती, ललकार और गर्जना के साथ बलिदान की भी मानसिकता नजर आती है। इन रचनाओं को राष्ट्रीय चेतना के रूप में प्रस्तुत करने में हमें तो कोई समस्या दिखाई नहीं देती। हां समस्या तो है, वो है आजादी के वास्तविक सरोकारों की खोज करने वाली रचनाओं के साथ। इसके उदाहरणस्वरू हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के वाक्य पर ध्यान दें तो सारी बातें साफ हो जाएंगी, ‘हमारा विशाल देश राष्ट्र की भावना या कल्पना से वैदिक युग से परिचित रहा है।’
सारांश…
राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में आधुनिक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रवाद से सामुदायिक भावना का विकास होता है और लोकतांत्रिक भावना भी राष्ट्रवाद से समृद्ध होती है। देश की रक्षा, हित, संगठन, एक समाज के जातीय स्वरूप के विकास की आकांक्षा, कोशिश राष्ट्रीय चेतना का अविभाज्य अंग है। अपनी संस्कृति के प्रति गौरव-बोध वस्तुत: राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा है और राष्ट्रीय अस्मिता राष्ट्रबोध का अभिन्न हिस्सा है। अज्ञेय का यह कथन युक्तियुक्त है, ‘संस्कृतियों का संबंध अपनी देशभूमि से होता है।’
भारतीय राष्ट्रवाद और हिन्दी साहित्य
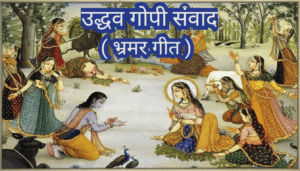







1 thought on “राष्ट्रवादी विचारधारा के साहित्यिक आयाम”