अंतस के आरेख
विषय : शिक्षा और रोजगार
दिनाँक : २४/०१/२०२०
शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्त्व का विकसित करने की एक प्रक्रिया है और यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की ‘शिक्ष्’ धातु में ‘अ’ प्रत्यय लगाने से बना है। ‘शिक्ष्’ का अर्थ है सीखना और सिखाना। ‘शिक्षा’ शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।
शिक्षा मे आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या आदि समाविष्ट हैं। एक पीढ़ी द्वारा अपने निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास ही शिक्षा है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है।
शिक्षा को हम दो भागों में विभक्त करके देखेंगे। पहला व्यापक रूप तथा दूसरा संकुचित रूप।
व्यापक रूप में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य पल-प्रतिपल नए-नए अनुभव प्राप्त करता रहता है। जिससे उसका प्रतिदन के आधार पर स्वभाव प्रभावित होता रहता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत स्वरूप को प्राप्त करता है।
संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों यानी विद्यालय, महाविद्यालय आदि में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। जहाँ शिक्षित होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करता है।
अब बात करते हैं शिक्षा और रोजगार के सम्बन्ध की…
सामान्यतः शिक्षा और रोजगार का आपस में कोई संबंध नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा का मूल प्रयोजन और उद्देश्य व्यक्ति की सोई शक्तियां जगाकर उसे सभी प्रकार से योग्य बनाना होता है। रोजगार की गारंटी देना शिक्षा का काम या उद्देश्य वास्तव में कभी नहीं रहा, यद्यपि आरंभ से ही व्यक्ति अपनी अच्छी शिक्षा के बूते पर रोजगार पाता आ रहा है। परंतु आज पढऩे-लिखने या शिक्षा पाने का अर्थ ही यह लगाया जाने लगा है कि ऐसा करके व्यक्ति रोजी-रोटी कमाने के योग्य बन सके। दूसरे शब्दों में आज शिक्षा का सीधा संबंध तो रोजगार के साथ जुड़ गया है, पर शिक्षा को अभी तक रोजगार परक नहीं बनाया जा सका है। आज जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, वह व्यक्ति को कुछ विषयों के नामादि स्मरण कराने या साक्षर बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती।
तात्पर्य यह है कि आमतौर पर स्कूल-कॉलेजों की वर्तमान शिक्षा रोजगार पाने में विशेष सहायक नहीं होती। या सबके लिए तो सहायक नहीं हो पा रही है।
स्कूल कालेजों में कुछ विषय रोजगारोन्मुख पढ़ाए जाते हें। कॉमर्स, साइंस आदि विषय ऐसे ही हैं, इनके बल पर रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। साइंस के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि के क्षेत्रों में अपनी शिक्षा को नया रूप देकर रोजगार के पर्याप्त अवसर पा जाते हैं। फिर और कई तरह के से भी आज तकनीकि-शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसे विस्तार भी दिया जा रहा है।
पॉलिटेकनिक, आई.टी.आई. जैसी संस्थांए इस दिशा में विशेष सक्रिय हैं। इनमें विभिन्न टेड्स या कामधंधों, दस्तकारियों से संबंधित तकनीकी शिक्षा दी जाती है। उसे प्राप्त कर व्यक्ति स्व-रोजगार योजना भी चला सकता है और विभिन्न प्रतिष्ठानों में अच्छे रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकता है। समस्या तो उनके लिए हुआ करती है, जिन्होंने शिक्षा के नाम पर केवल साक्षरता और उसके प्रमाण-पत्र प्राप्त किए होते हैं। निश्चय ही उन सबके लिए उनके बल पर रोजगार के अवसर इस देश में तो क्या, सारे विश्व में ही बहुत कम अथवा नहीं ही हैं।
व्यवहार के स्तर पर यों भी हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा दी गई घिसी-पिटी शिक्षा-प्रणाली चल रही है, वह अब देश-काल की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में समर्थ नहीं रह गई है। अत: उसमें सुधार करना अतिआवश्यक है। देश-विदेश में आज जो भिन्न प्रकार के तकनीक विकसित हो गए या हो रहे हैं, उन सबको शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। अब जब शिक्षा का उद्देश्य रोजगार पाना बन ही गया है तो पुरारे ढर्रे पर चल कर लोगों का धन, समय और शक्ति नष्ट करने, उन्हें मात्र साक्षर बनाकर छोड़ देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस शिक्षा प्रणाली को दूर करने अथवा बदलने के लिए यदि हमें वर्तमान शिक्षा-जगत का पूरा ढांचा भी क्यों न बदलना पड़े, बदल डालने से रुकना या घबराना नहीं चाहिए। यही समय की मांग है।
समय और परिस्थितियों के प्रभाव के कारण अब शिक्षा का अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति की सोई शक्तियां जगाकर उसे ज्ञानवान और समझदार बनाने तक ही सीमित नहीं रह गया है। बदली हुई परिस्थितियों में मनुष्य के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करना भी हो गया है। पर खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे देश में सर्वाधिक उपेक्षा का क्षेत्र शिक्षा ही है। सरकारी बजट में सबसे कम राशि शिक्षा के लिए ही रखी जाती है। शिक्षालय अभावों में पल रहे हैं। इसे स्वस्थ शिक्षा प्रणाली का परिचायक नहीं हो सकता।
और अंत में, इसके सुधारा के दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, शिक्षा और रोजगार को अलग अलग कर दें और दोनों पर अलग से फंड की व्यवस्था हो। जिससे शिक्षित समाज और स्थिर समाज का निर्माण हो सके, जिसमें शिक्षित नए नए शिक्षा औ। र रोजगार के मानदंड तैयार कर सके। और व्यवसाई वर्ग उन्हें अपनाकर रोजगार विकसित कर सके।
दूसरा, अगर शिक्षा और रोजगार को एक साथ जोड़ कर रखना जरूरी हो तो ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण हो जिसमें हर एक व्यक्ति शिक्षण संस्थानो से निकल कर भीड़ बनने के स्थान पर सीधे अपनी काबिलियत के अनुसार राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सके।
धन्यवाद !
अश्विनी राय ‘अरूण’



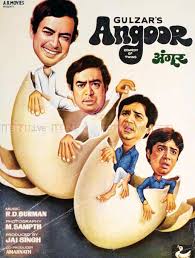


1 thought on “रोजगार परक शिक्षा”