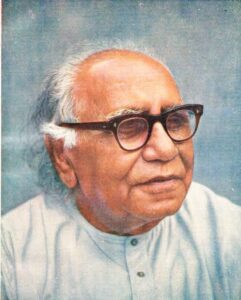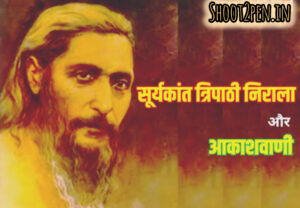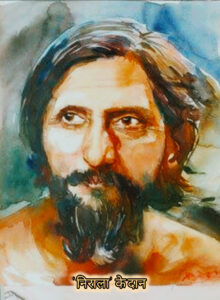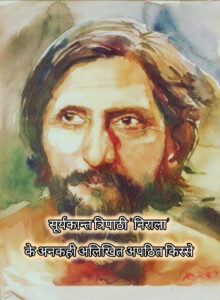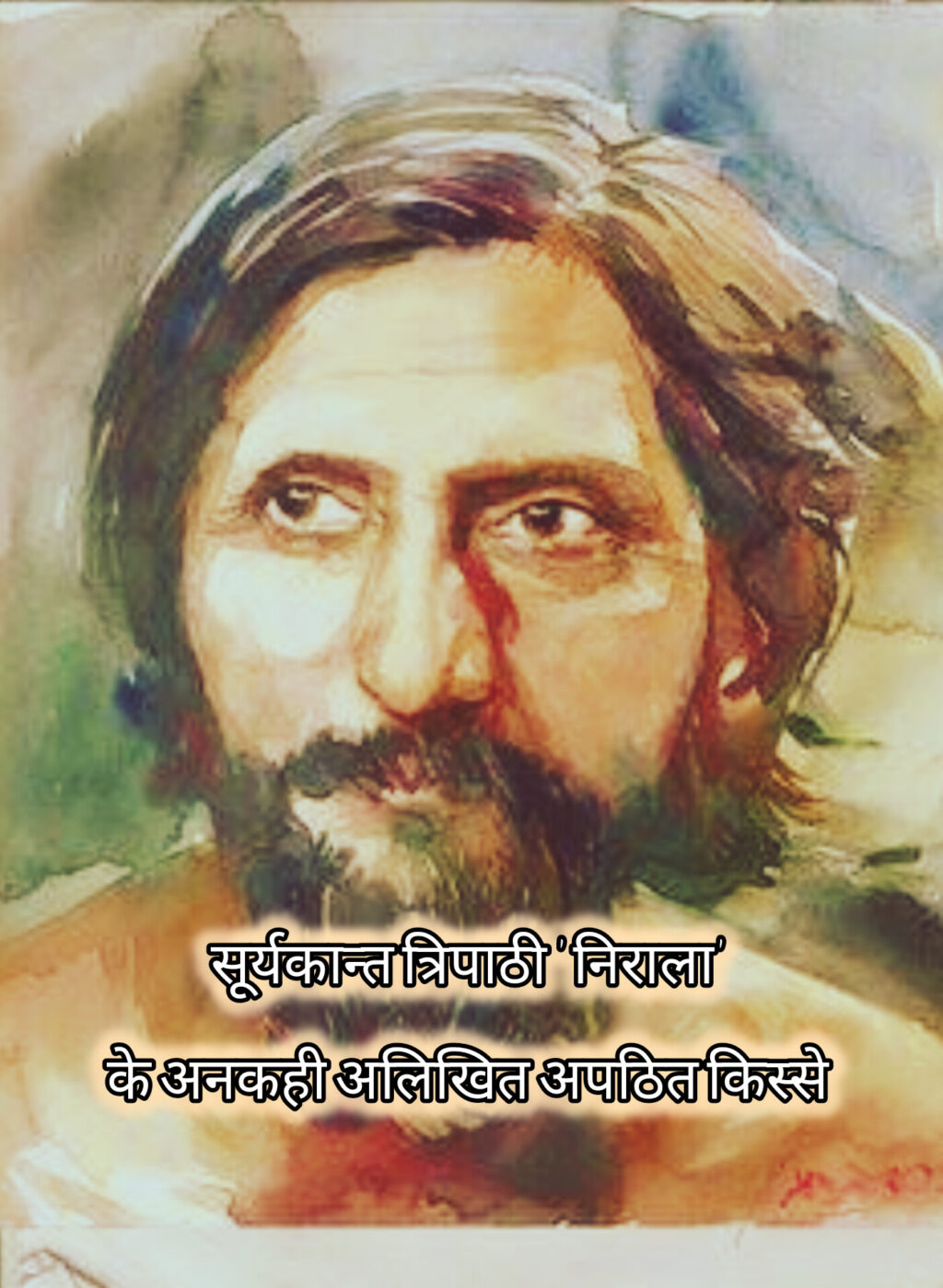
एक बार एक सज्जन को उनकी वर्षों की मेहनत के कुछ रुपए मिले थे, वो उन रुपयों को लेकर इक्के से इलाहाबाद की सड़क पर चले जा रहे थे। रास्ते में सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला हाथ पसार कर भीख मांग रही थी। उसे देख उन सज्जन ने इक्का रुकवाया और उनके पास गए, और पूछा – ‘ माई ! आज कितनी भीख मिली ?
बुढ़िया ने जवाब दिया -‘ सुबह से आज कुछ नहीं मिला बेटा !’
बुढ़िया के इस उत्तर को सुनकर सज्जन सोच में पड़ गए कि बेटे के रहते मां भीख मांग रही है। एक रुपैया बुढ़िया के हाथ पर रख कर बोले, ‘ मां अब कितने दिन भीख नहीं मांगोगी?
तीन दिन बेटा।
दस रुपये दे दूं तो…?
बीस या पच्चीस दिन।
सौ रुपये दे दूं तो…?
चार-पांच महीने तक!
चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे मां मांगती गई, बेटा देता गया। इक्के वाला हक्का-बक्का रह गया। बेटे की जेब हल्की होती गई और मां के भीख न मांगने की अवधि बढ़ती चली गई। जब सज्जन ने रुपयों की अंतिम ढेरी भी बुढ़िया की झोली में डाल दी तो बुढ़िया खुशी से चीख उठी और कहने लगी, “अब कभी भी नहीं मांगूंगी बेटा, कभी नहीं।”
सज्जन ने संतोष की सांस ली। बुढ़िया के पैर छुए। बुढ़िया ने उन्हें ढेरों आशीष और दुआएं दी।सज्जन इक्के में बैठकर अपने घर की राह पर चल दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब संतोष व फक्कड़ता का भाव था।
वैसे तो आप इलाहाबाद और फक्कड़ता शब्द को पढ़कर ही समझ गए होंगे कि वो सज्जन कौन थे, मगर हम अपनी संतुष्टि के लिए बताते चलें कि वो इलाहाबाद के फक्कड़ कोई और नहीं बल्कि महान साहित्यकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ जी थे। आज हम आपके सम्मुख कुछ ऐसी ही बातों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो निराला को अन्य महान साहित्यकारो से अलग करती है…
परिचय…
निराला का “फक्कड़ व्यक्तित्व” उनकी स्वाभिमानी, विद्रोही, और स्वच्छंद प्रकृति का प्रतीक था, जो सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक तंगी के बावजूद सिद्धांतों से समझौता न करने वाले साहसी भाव, गहन संवेदनशीलता, तथा विनोदप्रियता से युक्त था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, फिर भी उन्होंने कभी अपना आदर्श नहीं त्यागा और विषम परिस्थितियों में भी मानव मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखी।
गांधी का हिन्दी प्रेम…
हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए महात्मा गांधी का प्रेम जगजाहिर है, पर क्या आपको यह पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ से हिंदी की अस्मिता को लेकर बापू की भिड़ंत हो गई थी, और निराला ने अपनी खिन्नता को इतना विस्तार से लिखा कि बापू के आलोचक आजतक इसका इस्तेमाल करते हैं।
हुआ यह था कि गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में एक वक्तव्य दिया कि ‘इस मौके पर अपने दुख की भी कुछ कहानी कह दूं। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिंदी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिंदी बोलने वालों में रवीन्द्रनाथ कहां हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहां हैं? जगदीश बोस कहां हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा मात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं। लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है, उसमें ऐसे महान व्यक्तियों के होने की आशा रखी ही जायेगी।”
बस फिर क्या था, गांधी के इस बयान के बाद निराला भड़क गए और उन्होंने गांधी से मिलकर अपने मन की बात रखने की अनुमति चाही। काफी कोशिशों के बाद निराला को गांधी से मिलने का समय मिल गया, वह भी सिर्फ २० मिनट के लिए। निराला ने अपनी इस मुलाकात का विवरण स्वयं इन शब्दों में लिखा…
मैंने (गांधीजी से) कहा- आपके सभापति के अभिभाषण में हिंदी के साहित्य और साहित्यिकों के संबंध में, जहां तक मुझे स्मरण है, आपने एकाधिक बार पं बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम सिर्फ़ लिया है। इसका हिंदी के साहित्यिकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने सोचा था?
महात्माजी- मैं तो हिंदी कुछ भी नहीं जानता।
निराला- तो आपको क्या अधिकार है कि आप कहें कि हिंदी में रवींद्रनाथ ठाकुर कौन हैं?
महात्माजी- मेरे कहने का मतलब कुछ और था।
निराला- यानी आप रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा साहित्यिक हिंदी में नहीं देखना चाहते, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का नाती या नोबल-पुरस्कार प्राप्त मनुष्य देखना चाहते हैं, यह?
यह संवाद सुन वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लोग ताज्जुब से निराला की तरफ़ देखने लगे। निराला जी ने आगे लिखा है कि-
मैंने स्वस्थ-चित्त हो महात्माजी से कहा- बंगला मेरी वैसी ही मात्र-भाषा है, जैसे हिंदी। रवींद्रनाथ का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है। मैं आपसे आधा घंटा समय चाहता हूं। कुछ चीजें चुनी हुई रवींद्रनाथ की सुनाऊंगा, उनकी कला का विवेचन करूंगा, साथ कुछ हिंदी की चीजें सुनाऊंगा।
महात्माजी- मेरे पास समय नहीं है।
निरालाजी ने लिखा- ‘मैं हैरान होकर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति को देखता रहा, जो राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को रास्ता बतलाता है, बेमतलब पहरों तकली चलाता है, प्रार्थना में मुर्दे गाने सुनता है, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति है, लेकिन हिंदी के कवि को आधा घंटा वक्त नहीं देता- अपरिणामदर्शी की तरह जो जी में आता है, खुली सभा में कह जाता है, सामने बगलें झांकता है!
खैर, इस बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात में, गांधीजी के सामने अपनी बात रखने गए निराला, बड़े खिन्नन मन से वहां से लौटे। लौटने के बाद उन्होंने बापू के नाम यह कविता लिखी-
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि
तो क्या भजते होते तुमको
ऐरे-ग़ैरे नत्थू खैरे – ?
सर के बल खड़े हुए होते
हिंदी के इतने लेखक-कवि?
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि
तो लोकमान्य से क्या तुमने
लोहा भी कभी लिया होता?
दक्खिन में हिंदी चलवाकर
लखते हिंदुस्तानी की छवि,
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि?
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि
तो क्या अवतार हुए होते
कुल के कुल कायथ बनियों के?
दुनिया के सबसे बड़े पुरुष
आदम, भेड़ों के होते भी!
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि?
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि
तो क्या पटेल, राजन, टंडन,
गोपालाचारी भी भजते- ?
भजता होता तुमको मैं औ´
मेरी प्यारी अल्लारक्खी !
बापू, तुम मुर्गी खाते यदि !
जीने और जिलाने की कला…
एक बार मद्रासी युवक निराला से चादर मांगकर ले गया। निराला के मित्र पाठक जी ने कहा, ”यह (आदमी) आपकी चादर वापस नहीं करेगा। अभी दोपहर को गुदड़ी बाजार में आठ आने में बेच आएगा। निराला ने प्रतिवाद किया, ”हो सकता है, और इसकी बात भी सच हो सकती है। मद्रासी यह सोचकर अपने गांव से नहीं चला होगा कि मांगी हुई चादर गुदड़ी बाजार में बेचेगा।” निराला की अंतर्दृष्टि ने धोखा नहीं खाया। चादर वापस आ गयी।
दो महीने बाद वही मद्रासी युवक कांग्रेस के अधिवेशन की भीड़भाड़ में दूर से ही ऊंचे कदवाले अपने उस दाता को पहचान लेता है, दौड़कर वापस आता है, टूटी-फूटी हिंदी में अपना परिचय देता है। उसे कांग्रेस अधिवेशन में कुछेक दिनों के लिए स्वयंसेवक का धंधा मिल गया था।
वॉलंटियर की वर्दी में दोनों हाथ उठाकर युवक ने हर्षध्वनि की और लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं वही हूं जिसे आपने इलाहाबाद में चादर दी थी। निराला को लगा कला का जीवित रूप उनके सामने खड़ा है। उन्हें अपार हर्ष हुआ।
दो चार रोज बाद वह युवक फिर दिखाई दिया। अबकी उसने कहा, गरमी बहुत पड़ने लगी है। देश जाना चाहता हूं। रेल का किराया कहां मिलेगा। पैदल ही जाना पड़ेगा।
निराला ने पूछा, ”कांग्रेस वाले क्या आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते ?”
उसने कहा, ” नहीं, कांग्रेस का ऐसा नियम नहीं है। मैं मिला था। मुझे यही उत्तर मिला। खैर, मैं भीख-मांगता खाता पैदल चला जाऊंगा। अपने नंगे पैरों की ओर देखकर बोला, ”पर गरमी बहुत पड़ रही है। पैरों में फफोले पड़ जाएंगे। अगर एक जोड़ी चप्पल आप ले दें।”
निराला की छाती फट गयी यह सुनकर। उन्होंंने लिखा,”मैं लज्जा से वहीं गड़ गया। मेरे पास तब केवल छह पैसे थे। उतने में चप्पल नहींं आ सकती थी। अपनी चप्पलें देखीं, घिसी पुरानी थींं। लज्जित होकर बोले- आप मुझे क्षमा करें, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं।
इसके बाद मद्रासी युवक वीर-भाव से निराला को देखने लगा, फिर बड़े भाई की तरह उनसे आशीर्वाद लिया और मुस्कुराकर अमीनाबाद की ओर चला गया। निराला ने इस समूची घटना को लिखा और उसका शीर्षक दिया ”कला की रूपरेखा”। क्योंकि उनका चिंतन जीने और जिलाने की कला को श्रेष्ठ कला मानता था।
परिचय देने की कला…
एक समय की बात है। लखनऊ के एक ताल्लुकेदार ने कई गणमान्य कवियों को अपनी कोठी पर निमंत्रण भेजा। काव्य संध्या का आयोजन था। निराला को भी निमंत्रण गया। निराला इस तरह कहीं जाते नहीं थे। मगर जब दोस्तों ने जोर डाला तो निराला चले गए। आयोजन से पहले शाम को तालुकेदार साहब अपने मुंशी के साथ हाज़िर हुए। मुंशी एक एक करके सारे कवियों का परिचय तालुकेदार साहब से करवा रहा था और नंबर आने पर हर कवि अपनी जगह पर खड़ा होकर खुद को धन्य मानते हुए ये परिचय सुन रहा था। निराला को ये तरीक़ा पसंद नहीं आया।
उन्होने सोचा कि मुंशी क्यों परिचय करवा रहा है। ताल्लुकेदार को ख़ुद कवियों से उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए था। अगर नहीं है परिचय तो बुलाया ही क्यों। जब निराला का नंबर आया तो उन्होने मुंशी को परिचय देने से रोक दिया और खुद तालुकेदार को अपना परिचय देते हुए कहा- हम वो हैं जिनके दादा की पालकी को आपके दादा ने अपने कंधे पर ढोया था। सब लोग निराला का ये अंदाज़ सुनकर हक्के-बक्के रह गए। निराला का इशारा उस घटना की तरफ़ था जब महाकवि भूषण की पालकी को ख़ुद महाराज छत्रसाल ने उठाया था और इस तरह भूषण के कवित्त्व का सम्मान किया था। निराला ने जब ये घटना वहां मौजूद लोगों को याद दिलाई तो सब उनके तेवर के क़ायल हो गए।
हास्य विनोद…
इलाहाबाद में एक साहित्यकार थे, पंडित ज्योति प्रसाद मिश्र ‘निर्मल’। निराला के आत्मीय थे और उनसे निराला की दोस्ताना नोक-झोंक चलती रहती थी। एक बार निराला ने निर्मल से कहा- भई निर्मल ये तुमने अपने नाम में निर् निर् क्या लगा रखा है। इस पर निर्मल बोले- ये निर् तो आपके नाम में भी है। निराला को इसी मौक़े का इंतज़ार था। बोले- मेरे नाम से अगर निर् निकाल भी दो तब भी मैं आला रहूंगा। मगर तुम्हारे नाम से निर् निकाल दिया जाए तो सिर्फ़ मल बचेगा।
बनारस एक गर्व…
एक बार जयशंकर प्रसाद, बनारसीदास चतुर्वेदी और निराला जी बनारस में थे। बनारसीदास ने प्रसाद जी को सुनाते हुए कहा- बनारस में अब कुछ नहीं बचा है। ये पिछड़ा शहर है, लोग भी पिछड़े हैं। प्रसाद जी मेज़बान होने का धर्म निभाते हुए चुप रहे मगर निराला ने जवाब दिया कि चतुर्वेदी जी, बनारस का जलवा आप क्या जानें। बनारस की महिमा देखिए कि मां-बाप अपने बच्चों का नाम बनारसीदास रखना पसंद करते हैं।
अपनी बात…
निराला मस्तमौला, यायावर तो थे ही, फकीरी में भी दानबहादुरी ऐसी कि जेब का आखिरी आना-पाई तक गरीबों पर लुटा आते थे। नई रजाई-गद्दा रेलवे स्टेशन के भिखारियों को दान कर खुद कड़कती जाड़े में फटी रजाई तानकर सो जाते थे। जीवन की ऐसी विसंगतियां-उलटबासियां शायद ही किसी अन्य महान कवि-साहित्यकार की सुनने-पढ़ने को मिलें, जैसी की महाप्राण के बारे में सुनने-पढ़ने को मिलती है। सुख-दुख की कई अनकही-अलिखित-अपठित गाथाएं निराला जी के जीवन से जुड़ी हैं, जिसके बारे में हम आगे के आलेख में पढ़ेंगे…