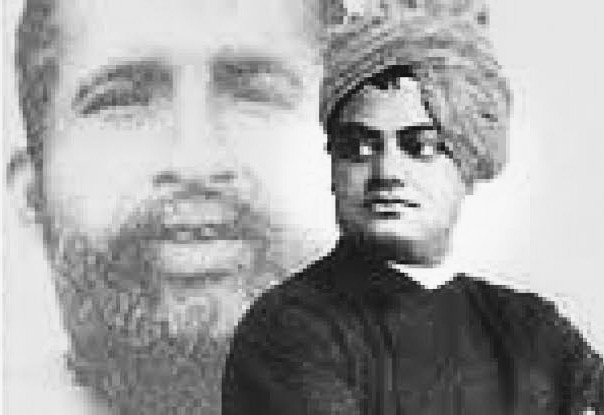
युवावस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद्व से गुज़रना पड़ा। परमहंस जी जैसे जौहरी ने रत्न को परखा। उन दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने नरेन्द्र को बदल दिया। इसी समय उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परमसत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं, बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेन्द्र उन्मत्त-से रहे। उन्हें गुरु ने आत्मदर्शन करा दिया था। पच्चीस वर्ष की अवस्था में नरेन्द्र दत्त ने काषायवस्त्र धारण किये। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र ने संन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। जीवन के आलोक को जगत के अन्धकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित करना था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की।
निष्ठा…
एक दिन की बात है, किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक-भौं सिकोड़ीं। यह देखकर विवेकानन्द को क्रोध आ गया। वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भण्डार की महक फैला सके। ऐसी थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरुभक्ति, गुरुसेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। स्वामी विवेकानन्द अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यन्त रुग्ण हो गया था। गुरुदेव के शरीर-त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुम्ब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिन्ता किये बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे।
विवेकानन्द बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदान्त के सिद्धान्तों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धान्त का जो आधार विवेकानन्द ने दिया उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूँढा जा सके। विवेकानन्द को युवकों से बड़ी आशाएँ थीं। आज के युवकों के लिये इस ओजस्वी संन्यासी का जीवन एक आदर्श है।
राष्ट्र र्निर्माण…
स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं को हिमालय में चिंतनरूपी आनंद सागर में डुबाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी ही वह इसे त्यागकर भारत की कारुणिक निर्धनता से साक्षात्कार करने और राष्ट्र र्निर्माण के लिए समूचे भारत में भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा। इन छ्ह वर्षों के भ्रमण काल में वह राजाओं और दलितों, दोनों के अतिथि रहे। उनकी यह महान् यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई, जहाँ ध्यानमग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर रुझान वाले नए भारतीय वैरागियों और सभी आत्माओं, विशेषकर जनसाधारण की सुप्त दिव्यता के जागरण से ही इस मृतप्राय देश में प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः वर्ष १८९३ में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहाँ वह बिना आमंत्रण के गए थे, परिषद में उनके प्रवेश की अनुमति मिलनी ही कठिन हो गयी। उनको समय न मिले, इसका भरपूर प्रयत्न किया गया। भला, पराधीन भारत क्या सन्देश देगा- योरोपीय वर्ग को तो भारत के नाम से ही घृणा थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर के उद्योग से किसी प्रकार समय मिला और ११ सितंबर, वर्ष १८९३ के उस दिन उनके अलौकिक तत्वज्ञान ने पाश्चात्य जगत को चौंका दिया। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि वस्तुत: भारत ही जगद्गुरु था और हमेशा रहेगा। स्वामी विवेकानन्द ने वहाँ भारत और हिन्दू धर्म की भव्यता स्थापित करके ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ा। ‘सिस्टर्स ऐंड ब्रदर्स ऑफ़ अमेरिका’ (अमेरिकी बहनों और भाइयो) के संबोधन के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते ही ७००० प्रतिनिधियों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। विवेकानंद ने वहाँ एकत्र लोगों को सभी मानवों की अनिवार्य दिव्यता के प्राचीन वेदांतिक संदेश और सभी धर्मों में निहित एकता से परिचित कराया। वर्ष १८९६ तक वे अमेरिका में रहे। उन्हीं का व्यक्तित्व था, जिसने भारत एवं हिन्दू-धर्म के गौरव को प्रथम बार विदेशों में जागृत किया। धर्म एवं तत्वज्ञान के समान भारतीय स्वतन्त्रता की प्रेरणा का भी उन्होंने नेतृत्व किया। स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे, ‘मैं कोई तत्ववेत्ता नहीं हूँ। न तो संत या दार्शनिक ही हूँ। मैं तो ग़रीब हूँ और ग़रीबों का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो सच्चा महात्मा उसे ही कहूँगा, जिसका हृदय ग़रीबों के लिये तड़पता हो।’
पाँच वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों, लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की भी यात्राएं कीं। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। कुछ अवसरों पर वह चरम अवस्था में पहुँच जाते थे, यहाँ तक कि पश्चिम के भीड़ भरे सभागारों में भी। यहाँ उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया और उनमें से कुछ को अमेरिका के ‘थाउज़ेंड आइलैंड पार्क’ में आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित किया। उनके कुछ शिष्यों ने उनका भारत तक अनुसरण किया। स्वामी विवेकानन्द ने विश्व भ्रमण के साथ उत्तराखण्ड के अनेक क्षेत्रों में भी भ्रमण किया जिनमें अल्मोड़ा तथा चम्पावत में उनकी विश्राम स्थली को धरोहर के रूप में सुरक्षित किया गया है।






