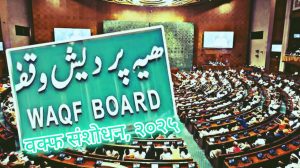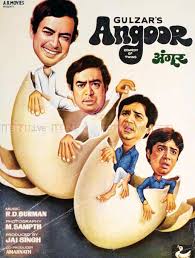आज हम हिन्दी साहित्य पर चर्चा करते हैं। हिन्दी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती हैं। परंतु हिन्दी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती हैं। हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से जो कि ज्यादातर लोकभाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में तीन प्रकार के साहित्य हैं। गद्य पद्य और चम्पू। हिंदी की पहली रचना कौन सी है उसे किसने लिखी है यह एक विवाद का विषय है तो इस विषय को अभी जाने देते हैं…
हिन्दी साहित्य के विकास को हम अपनी सुविधा के लिये पाँच ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर के देखते हैं, पहला आदिकाल का हिन्दी साहित्य जिसे हम १४वीं ई. से पहले का मान सकते हैं, दूसरा भक्ति काल जो १३७५ – १७०० के मध्य में, तीसरा रीति काल जो की १७०० – १९०० के मध्य में पड़ता है, चौथा आधुनिक काल १८५० ई. के पश्चात और नव्योत्तर काल जिसे हम १९८० ई. के पश्चात से अभी तक के समय काल को मान सकते हैं।
अभी के लिए हम सिर्फ आधुनिक काल को ही लेते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ -साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। यही वह समय था जब हिन्दी साहित्य में छायावाद की एक नई विधा ने जन्म लिया। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य -धारा है जो लगभग १९१८ से १९३६ तक की प्रमुख युगवाणी रही।छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पाण्डेय को जाता है। आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा बिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रा नंद पंत, महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावादी युग के ये चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं…
श्री जयशंकर प्रसाद जी
प्रसाद जी का जन्म ३० जनवरी १८८९, दिन – गुरुवार को काशी के सरायगोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवीप्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिये विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशीनरेश के बाद ‘हर हर महादेव’ से बाबू देवीप्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण १७ वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुबिंयों, परिवार से संबद्ध अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सबका सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कालेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहाँ संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान् इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में ‘रसमय सिद्ध’ की भी चर्चा की जाती है।
प्रसाद जी के जीवनकाल में ऐसे साहित्यकार काशी में विधमान थे जिन्होंने अपनी कृतियों द्वारा हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। उनके बीच रहकर प्रसाद जी ने भी अनन्य गौरवशाली साहित्यों की रचना की। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक ओर निबंध, साहित्य की प्राय: सभी विधाओं में उन्होंने ऐतिहासिक महत्व की रचनाएँ कीं तथा खड़ी बोली की श्रीसंपदा को महान् और मौलिक दान से समृद्ध किया।
प्रसाद ने काव्यरचना वतपरचनब्रजभाषा में आरंभ की और धीर-धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भाँति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई।
कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभयिता माने जाते हैं। सन् 1912 ई. में ‘इंदु’ में उनकी पहली कहानी ‘ग्राम’ प्रकाशित हुई। प्राय: तभी से गतिपूर्वक आधुनिक कहानियों की रचना हिंदी में आरंभ हुई। प्रसाद जी ने कुल ७२ कहानियाँ लिखी हैं। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। कहानियों के साथ ही प्रसाद जी ने तीन उपन्यास लिखे। ‘कंकाल’, में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है। ‘तितली’ में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। प्रथम यथार्थवादी उन्यास हैं ; दूसरे में आदर्शोन्मुख यथार्थ है। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी हिंदी में यथार्थवादी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित करते हैं। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्राम, नगर, प्रकृति और जीवन का मार्मिक चित्रण किया है जो भावुकता और कवित्व से पूर्ण होते हुए भी प्रौढ़ लोगों की शैल्पिक जिज्ञासा का समाधान करता है।
प्रसाद जी ने आठ ऐतिहासिक, तीन पौराणिक और दो भावात्मक, कुल १३ नाटकों की सर्जना की। ‘कामना’ और ‘एक घूँट’ को छोड़कर ये नाटक मूलत: इतिहास पर आधृत हैं। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर संस्थित है। इन सबके अलावा प्रसाद जी ने प्रारंभ में समय समय पर ‘इंदु’ में विविध विषयों पर सामान्य निबंध भी लिखे। बाद में उन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध, यथा: सम्राट् चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यवर्त और उसका प्रथम सम्राट् आदि: भी लिखे हैं। ये उनकी साहित्यिक मान्यताओं की विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते हैं। विचारों की गहराई, भावों की प्रबलता तथा चिंतन और मनन की गंभीरता के ये जाज्वल्य प्रमाण हैं।
जहां प्रसाद जी की चर्चा हो और उनकी श्रेष्ट रचना कामायनी की चर्चा ना हो यह कैसे संभव हो सकता है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। ‘प्रसाद’ जी की यह अंतिम काव्य रचना १९३६ में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन प्राय: ७-८ वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। ‘चिंता’ से प्रारंभ कर ‘आनंद’ तक १५ सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। उन्हें ‘कामायनी’ पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उन्होंने जीवन में कभी साहित्य को अर्जन का माध्यम नहीं बनाया, अपितु वे साधना समझकर ही साहित्य की रचना करते रहे। कुल मिलाकर ऐसी बहुआयामी प्रतिभा का साहित्यकार हिंदी में कम ही मिलेगा जिसने साहित्य के सभी अंगों को अपनी कृतियों से न केवल समृद्ध किया हो, बल्कि उन सभी विधाओं में काफी ऊँचा स्थान भी रखता हो।
संस्करण…
हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभो समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ प्रतिज्ञा सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढे चलो बढे चलो
असंख्य कीर्ति रश्मियाँ, विकीर्ण दिव्य दाह सी सपूत मात्रभूमि के, रुको न शूर साहसी
अराती सैन्य सिन्धु में, सुवाढ़ वाग्नी से जलो प्रवीर हो जयी बनो, बढे चलो बढे चलो।
कालक्रम के अनुसार ‘चित्राधार’ प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण वर्ष १९१८ ई. में हुआ। इसमें कविता, कहानी, नाटक, निबन्ध सभी का संकलन था और भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों थी। लगभग दस वर्ष के बाद १९२८ में जब इसका दूसरा संस्करण आया, तब इसमें ब्रजभाषा की रचनाएँ ही रखी गयीं। साथ ही इसमें प्रसाद जी की आरम्भिक कथाएँ भी संकलित हैं। ‘चित्राधार’ की कविताओं को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक खण्ड उन आख्यानक कविताओं अथवा कथा काव्यों का है, जिनमें प्रबन्धात्मकता है। अयोध्या का उद्धार, वनमिलन, और प्रेमराज्य तीन कथाकाव्य इसमें संग्रहीत हैं। ‘अयोध्या का उद्धार’ में लव द्वारा अयोध्या को पुन: बसाने की कथा है। इसकी प्रेरणा कालिदास का ‘रघुवंश’ है। ‘वनमिलन’ में ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम’ की प्रेरणा है। ‘प्रेमराज्य’ की कथा ऐतिहासिक है। ‘चित्रधार’ की स्फुट रचनाएँ प्रकृतिविषयक तथा भक्ति और प्रेमसम्बन्धिनी है। ‘कानन कुसुम’ प्रसाद की खड़ीबोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। यद्यपि इसके प्रथम संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली दोनों की कविताएँ हैं, पर दूसरे संस्करण (१९१८ ई.) तथा तीसरे संस्करण (१९२९ ई.) में अनेक परिवर्तन दिखायी देते हैं और अब उसमें केवल खड़ीबोली की कविताएँ हैं। कवि के अनुसार यह सन् १९०९ ई. से 1974 वि. सन् १९१७ ई. तक की कविताओं का संग्रह है। इसमें भी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखी गयी कुछ कविताएँ हैं।
रचनाएँ…
प्रसाद जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है…
कामायनी : कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अक्षय कीर्ति का स्तम्भ है। भाषा, शैली और विषय-तीनों ही की दृष्टि से यह विश्व-साहित्य का अद्वितीय ग्रन्थ है। ‘कामायनी’ में प्रसादजी ने प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया है तथा मानव जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के समन्वित जीवन-दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की है।
आँसू : आँसू कवि के मर्मस्पर्शी वियोगपरक उदगारों का प्रस्तुतीकरण है।
लहर : यह मुक्तक रचनाओं का संग्रह है।
झरना : प्रसाद जी की छायावादी शैली में रचित कविताएँ इसमें संग्रहीत हैं।
चित्राधार : चित्राधार प्रसाद जी की ब्रज में रची गयी कविताओं का संग्रह है
गद्य रचनाएँ…
प्रसाद जी की प्रमुख गद्य रचनाएँ निम्नवात हैं…
नाटक : चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कन्दगुप्त, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूँट, विशाख, अजातशत्रु आदि।
कहानी-संग्रह : प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आँधी तथा इन्द्रजाल आपके कहानी संग्रह हैं।
उपन्यास : तितली और कंकाल।
निबन्ध : काव्य और कला।
अन्य रचनाएँ : अन्य कविताओं में विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएँ हैं। ‘कानन कुसुम’ में प्रसाद ने अनुभूति और अभिव्यक्ति की नयी दिशाएँ खोजने का प्रयत्न किया है। इसके अनन्तर कथाकाव्यों का समय आया है। ‘प्रेम पथिक’ का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले ‘इन्दू’ (१९०९ ई.) में प्रकाशित हुआ था और कवि ने इसे खड़ीबोली में रूपान्तरित किया। इसकी विज्ञप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है कि “यह काव्य ब्रजभाषा में आठ वर्ष पहले मैंने लिखा था।” ‘प्रेम पथिक’ में एक भावमूलक कथा है। जिसके माध्यम से आदर्श प्रेम की व्यंजना की गयी है।
प्रकाशन…
‘करुणालय’ की रचना गीतिनाट्य के आधार पर हुई है। इसका प्रथम प्रकाशन ‘इन्दु’ (१९१३ ई.) में हुआ। ‘चित्राधार’ के प्रथम संस्करण में भी यह है। १९२८ ई. में इसका पुस्तक रूप में स्वतन्त्र प्रकाशन हुआ। इसमें राजा हरिश्चन्द्र की कथा है। ‘महाराणा का महत्त्व’ १९१४ ई. में ‘इन्दु’ में प्रकाशित हुआ था। यह भी ‘चित्राधार’ में संकलित था, पर १९२८ ई. में इसका स्वतन्त्र प्रकाशन हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की कथा है। ‘झरना’ का प्रथम प्रकाशन १९१८ में हुआ था। आगामी संस्करणों में कुछ परिवर्तन किए गए। इसकी अधिकांश कविताएँ १९१४ से १९१७ के बीच लिखी गयीं, यद्यपि कुछ रचनाएँ बाद की भी प्रतीत होती हैं। ‘झरना’ में प्रसाद के व्यक्तित्व का प्रथम बार स्पष्ट प्रकाशन हुआ है और इसमें आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों को अधिक मुखर रूप में देखा जा सकता है। इसमें छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है। ‘आँसू’ प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण १९२५ ई. में निकला था। दूसरा संस्करण १९३३ ई. में प्रकाशित हुआ। ‘आँसू’ एक श्रेष्ठ गीतिकाव्य है, जिसमें कवि की प्रेमानुभूति व्यजित है। इसका मूलस्वर विषाद का है। पर अन्तिम पंक्तियों में आशा-विश्वास के स्वर हैं। ‘लहर’ में प्रसाद की सर्वोत्तम कविताएँ संकलित हैं। इसमें कवि की प्रौंढ़ रचनाएँ हैं। इसका प्रकाशन १९३३ ई. में हुआ। ‘कामायनी’ प्रसाद का निबन्ध काव्य है। इसका प्रथम संस्करण १९३६ ई. में प्रकाशित हुआ था। कवि का गौरव इस महाकाव्य की रचना से बहुत बढ़ गया। इसमें आदि मानव मनु की कथा है, पर कवि ने अपने युग के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है।
प्रसाद जी के काव्य की भावपक्षीय तथा कलापक्षीय विशेषताएँ निम्नवत् हैं…
भाव पक्ष…
बीती विभावरी जाग री!
अम्बर पनघट में डुबो रही
तारा घट ऊषा नागरी।
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा
किसलय का अंचल डोल रहा
लो यह लतिका भी भर लाई
मधु मुकुल नवल रस गागरी।
अधरों में राग अमंद पिये
अलकों में मलयज बंद किये
तू अब तक सोई है आली
आँखों में भरे विहाग री।
प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल क्षेत्र समाहित हुआ है। प्रेम, सौन्दर्य, देश-प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों को अभिनव और आकर्षक भंगिमा के साथ आपने काव्यप्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये सभी विषय कवि की शैली और भाषा की असाधारणता के कारण अछूते रूप में सामने आये हैं। प्रसाद जी के काव्य साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा और भव्यता बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। आपके नाटकों के गीत तथा रचनाएँ भारतीय जीवन मूल्यों को बड़ी शालीनता से उपस्थित करती हैं। प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को अपने साहित्य में सर्वत्र स्थान दिया है। आपकी अनेक रचनाएँ राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली हैं। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रकृति के सौम्य-सुन्दर और विकृत-भयानक, दोनों स्वरूप उनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं।
इसके अतिरिक्त प्रकृति का आलंकारिक, मानवीकृत, उद्दीपक और उपदेशिका स्वरूप भी प्रसादजी के काव्य में प्राप्त होता है। ‘प्रसाद’ प्रेम और आनन्द के कवि हैं। प्रेम-मनोभाव का बड़ा सूक्ष्म और बहुविध निरूपण आपकी रचनाओं में हुआ है। प्रेम का वियोग-पक्ष और संयोग-पक्ष, दोनों ही पूर्ण छवि के साथ विद्यमान हैं। ‘आँसू’ आपका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। उसके एक-एक छन्द में विरह की सच्ची पीड़ा का चित्र विद्यमान है; यथा-
जो धनीभूत पीड़ा थी,
मस्तक में स्मृति-सी छायी।
दुर्दिन में आँसू बनकर,
वह आज बरसने आयी।।
प्रसाद जी का सौन्दर्य वर्णन भी सजीव, सटीक और मनमोहक होता है। श्रद्धा के सौन्दर्य का एक शब्द चित्र दर्शनीय है-
नील परिधान बीच सुकुमार,
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल,
मेघ-वन बीच गुलाबी रंग।।
‘प्रसाद’ हिन्दी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। ‘आँसू’ और ‘कामायनी’ आपके छायावादी कवित्व के परिचायक हैं। छायावादी काव्य की सभी विशेषताएँ आपकी रचनाओं में प्राप्त होती हैं।
प्रसाद जी भावों के तीव्रता और मूर्तता प्रदान करने के लिए प्रतीकों का सटीक प्रयोग करते हैं। प्रसाद का काव्य मानव जीवन को पुरुषार्थ और आशा का संदेश देता है। प्रसाद का काव्य मानवता के समग्र उत्थान और चेतना का प्रतिनिधि है। उसमें मानव कल्याण के स्वर हैं। कवि ‘प्रसाद’ ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध, गौरवमय स्वरूपों के अभिनव चित्र उपस्थित किए हैं।
कला पक्ष…
‘प्रसाद’ के काव्य का कलापक्ष भी पूर्ण सशक्त और संतुलित है। उनकी भाषा, शैली, अलंकरण, छन्द-योजना, सभी कुछ एक महाकवि के स्तरानुकूल हैं।
भाषा…
प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आपने आरम्भ ब्रजभाषा से किया और फिर खड़ीबोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौन्दर्य से भी समन्वित है; यथा-
खग कुल कुल कुल-सा बोल रहा,
किसलय का अंचल डोल रहा।
प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौन्दर्य की सृष्टि की है।
शैली…
प्रसाद जी की काव्य शैली में परम्परागत तथा नव्य अभिव्यक्ति कौशल का सुन्दर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद-तीनों गुणों की सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि शैली-रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णनात्मक शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है।
अलंकरण…
प्रसाद जी की दृष्टि साम्यमूलक अलंकारों पर ही रही है। शब्दालंकार अनायास ही आए हैं। रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक आदि आपके प्रिय अलंकार हैं।
छन्द…
प्रसाद जी ने विविध छन्दों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। भावानुसार छन्द-परिवर्तन ‘कामायनी’ में दर्शनीय है। ‘आँसू’ के छन्द उसके विषय में सर्वधा अनुकूल हैं। गीतों का भी सफल प्रयोग प्रसादजी ने किया है। भाषा की तत्समता, छन्द की गेयता और लय को प्रभावित नहीं करती है। ‘कामायनी’ के शिल्पी के रूप में प्रसादजी न केवल हिन्दी साहित्य की अपितु विश्व साहित्य की विभूति हैं। आपने भारतीय संस्कृति के विश्वजनीन सन्दर्भों को प्रस्तुत किया है तथा इतिहास के गौरवमय पृष्ठों को समक्ष लाकर हर भारतीय हृदय को आत्म-गौरव का सुख प्रदान किया है। हिन्दी साहित्य के लिए प्रसाद जी माँ सरस्वती का प्रसाद हैं।
छायावाद…
जयशंकर प्रसाद ने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावादी पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखनेवाले श्रेष्ठ कवि भी बने। काव्यक्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार ‘कामायनी’ है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथाकाव्य भी है जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा (बुद्धि) के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावाद ओर खड़ी बोली की काव्यगरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानन्दन पंत इसे ‘हिंदी में ताजमहल के समान’ मानते हैं। शिल्पविधि, भाषासौष्ठव एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती है। जयशंकर प्रसाद ने अपने दौर के पारसी रंगमंच की परंपरा को अस्वीकारते हुए भारत के गौरवमय अतीत के अनमोल चरित्रों को सामने लाते हुए अविस्मरनीय नाटकों की रचना की। उनके नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि में स्वर्णिम अतीत को सामने रखकर मानों एक सोये हुए देश को जागने की प्रेरणा दी जा रही थी। उनके नाटकों में देशप्रेम का स्वर अत्यंत दर्शनीय है और इन नाटकों में कई अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध गीत मिलते हैं। ‘हिमाद्रि तुंग शृंग से’, ‘अरुण यह मधुमय देश हमारा’ जैसे उनके नाटकों के गीत सुप्रसिद्ध रहे हैं।